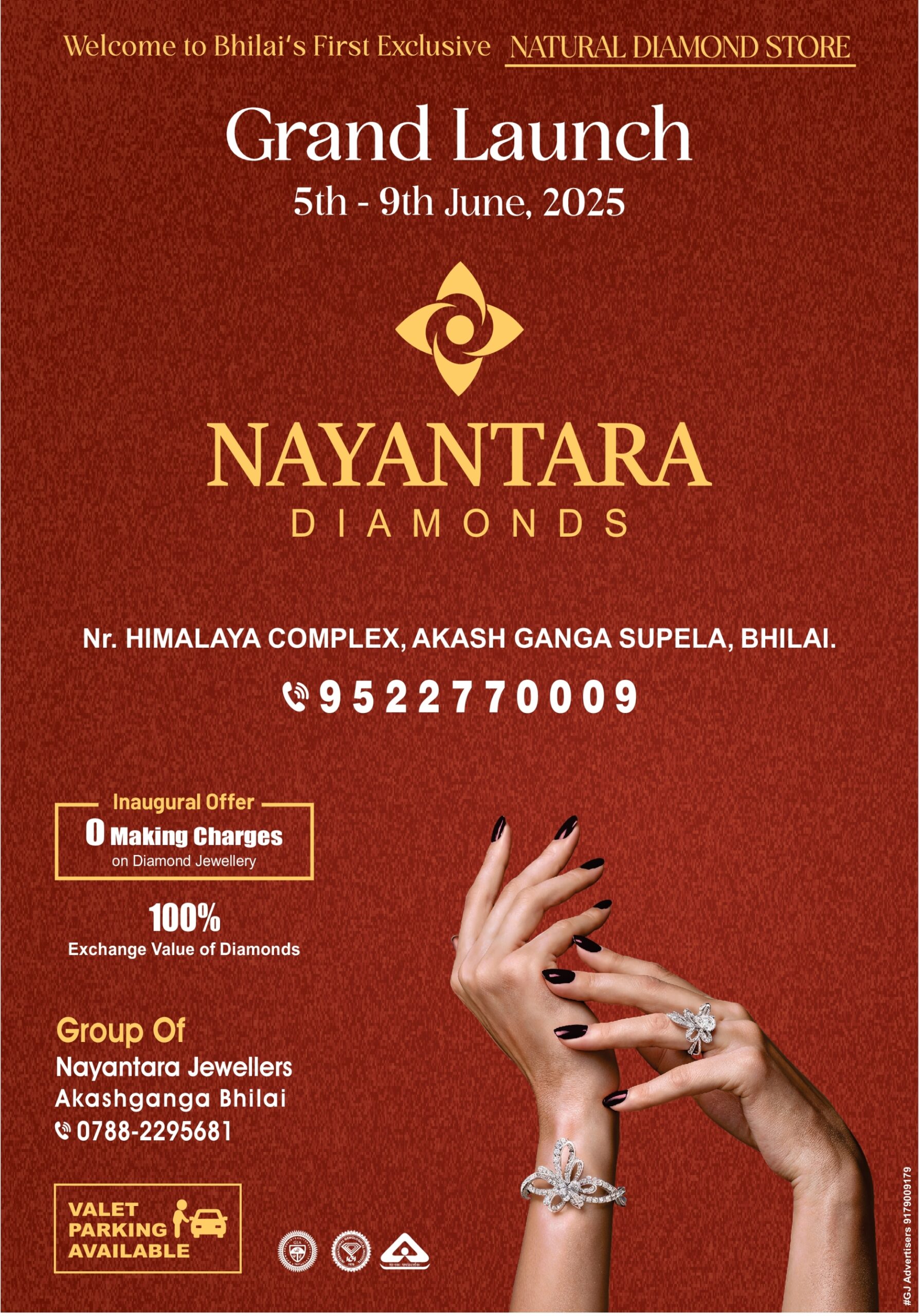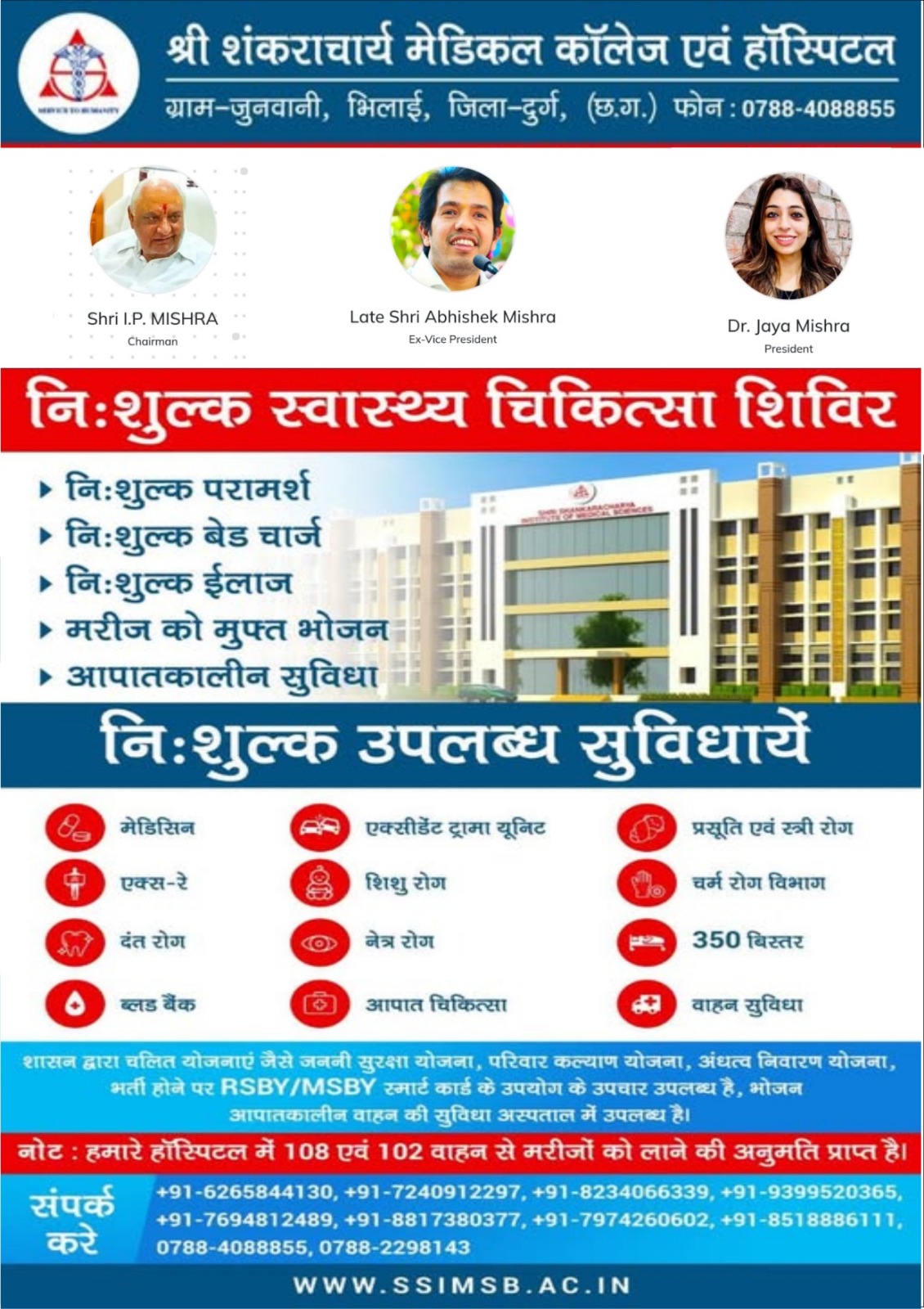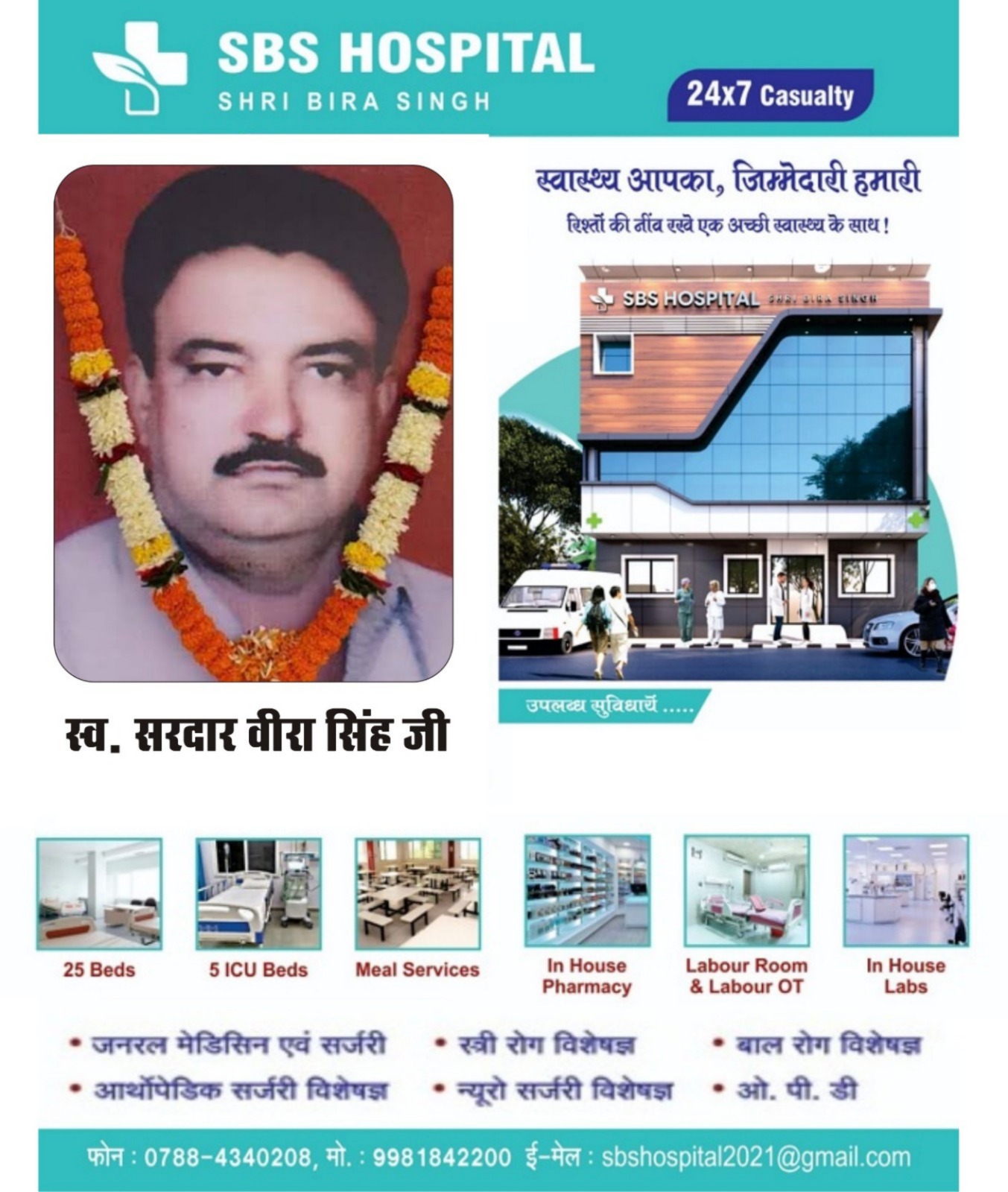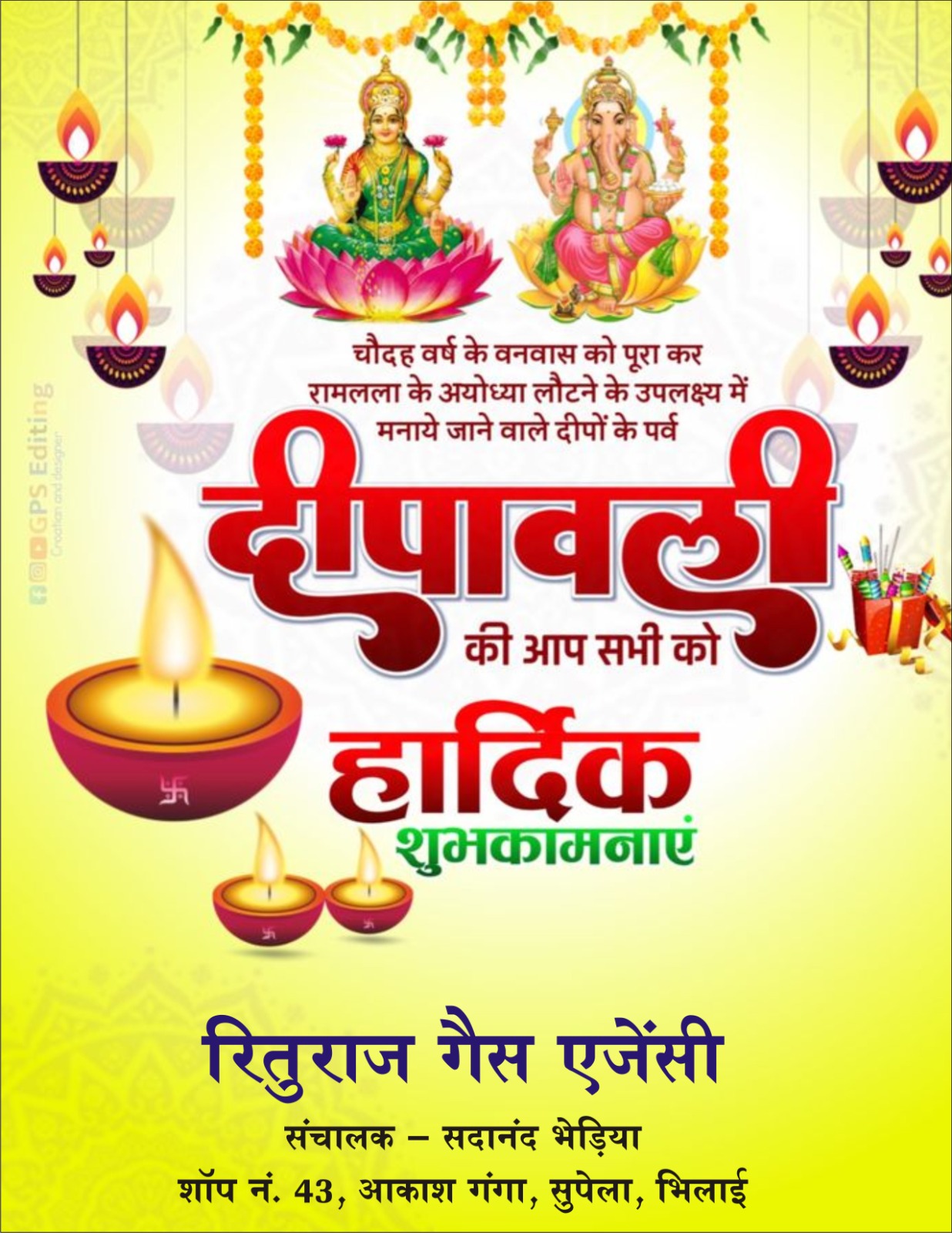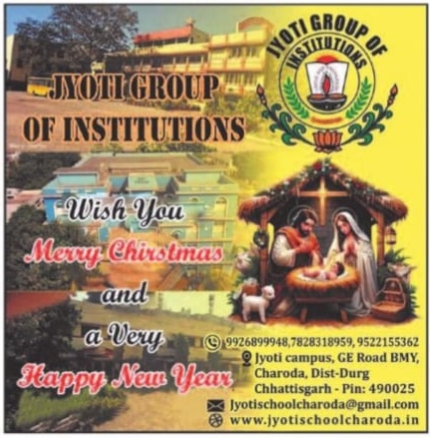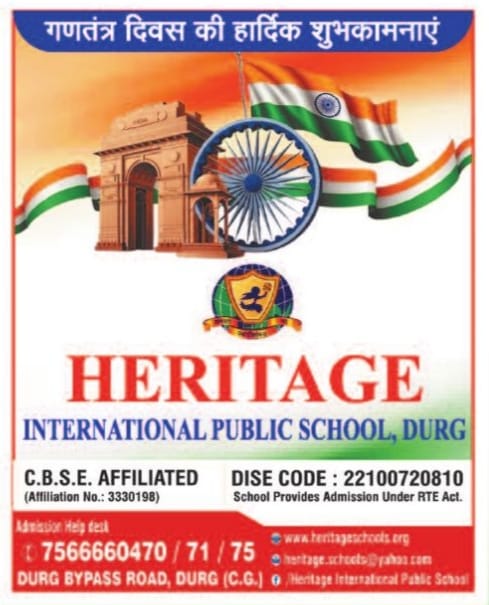विश्व जैव ईंधन दिवस प्रतिवर्ष 10 अगस्त को जैव ईंधन के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है, जो पशु अपशिष्ट, शैवाल और औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट से उत्पन्न होते हैं। जैव ईंधन, जीवाश्म ईंधन के विपरीत, कम समय में उत्पन्न होते हैं और तरल या गैसीय होते हैं। वे पर्यावरण के अनुकूल, टिकाऊ, नवीकरणीय और बायोडिग्रेडेबल हैं। आइए, हम विश्व जैव ईंधन दिवस के इतिहास, भारत में उपयोग किए जाने वाले जैव ईंधन के प्रकार, विश्व जैव ईंधन दिवस का महत्व और इस वर्ष के लिए इसकी थीम के बारे में जानते हैं।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा हर साल 10 अगस्त को World Biofuel Day यानि विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में नया जाता है. विश्व जैव ईंधन दिवस को ईंधन के अपरम्परागत स्रोतों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है. ऐसे जीवाश्म स्रोत जो ईंधन के विकल्प के रूप में काम कर सकते हैं. जैव ईंधन को ऊर्जा के किसी भी स्रोत जो जैविक सामग्री हो जैसे कृषि अपशिष्ट, फसल, पेड़ या घास से निकाला जाता है. कार्बन के किसी भी स्रोत से जैव ईंधन का उत्पादन किया जा सकता है. पारम्परिक जीवाश्म ईंधन की तुलना में जैव ईंधन में सल्फर नहीं होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड और विषाक्त उत्सर्जन भी कम होता है. आइए विश्व जैव ईंधन दिवस पर इसके महत्त्व , इतिहास और इस वर्ष की थीम जैसी महत्त्वपूर्ण जानकारी इस लेख से प्राप्त करते हैं।
जैव ईंधन क्या हैं?
यह पर्यावरण के अनुकूल ईंधन हैं जो नवीकरणीय बायो-मास संसाधनों से प्राप्त होते हैं। जैव ईंधन के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी के बारे में वैश्विक चिंताओं का समाधान होगा।पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण वे सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक लाभ प्रदान करते हैं । वे परिवहन ईंधन की तेजी से बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के पूरक हैं।लाभ : जैव ईंधन के उपयोग से कच्चे तेल पर आयात निर्भरता में कमी, स्वच्छ पर्यावरण, किसानों को अतिरिक्त आय और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन किया जा सकता है। जैव ईंधन कार्यक्रम मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत और किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की पहल के साथ तालमेल में है।
भारत में महत्वपूर्ण जैव ईंधन श्रेणियां
बायो-एथेनॉल : चीनी युक्त सामग्री, स्टार्च युक्त सामग्री और सेल्यूलोसिक सामग्री बायोमास से उत्पादित इथेनॉल।
बायो-डीजल : गैर-खाद्य वनस्पति तेलों, एसिड तेल, प्रयुक्त खाना पकाने के तेल/पशु वसा और जैव-तेल से उत्पादित फैटी एसिड का मिथाइल या एथिल एस्टर।
बायो-सीएनजी : यह बायो-गैस का शुद्ध रूप है जिसकी ऊर्जा क्षमता और संरचना जीवाश्म आधारित प्राकृतिक गैस के समान है।
विश्व जैव ईंधन दिवस
यह पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर-जीवाश्म ईंधन के महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये मनाया जाता है। ‘संयुक्त राष्ट्र विकास औद्योगिक संगठन’ और ‘वैश्विक पर्यावरण सुविधा (एक वित्तीय तंत्र) के सहयोग से ‘नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय’ ने इस अवसर पर निम्नलिखित दो योजनाएँ शुरू की हैं:
* इंटरेस्ट सबवेंशन योजना।
* जैविक अपशिष्ट स्ट्रीम्स का GIS आधारित इन्वेंटरी टूल।
जैव ईंधन कार्यक्रम भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के लिये भी महत्त्वपूर्ण है।
विश्व जैव ईंधन दिवस का इतिहास
ये दिवस सर रुडॉल्फ डीजल के किए अनुसंधान प्रयोग के सम्मान में मनाया जाता है. 1853 में, उन्होंने मूंगफली के तेल से ईंजन चलाया. उनके प्रयोग ने बाद की सदी में विभिन्न यांत्रिक इंजनों को ईंधन देने के लिए जीवाश्म ईंधन की जगह सब्जी के तेल का दरवाजा खोला।
विश्व जैव ईंधन दिवस का महत्व क्या है?
कोई भी हाइड्रोकार्बन ईंधन, जो किसी कार्बनिक पदार्थ (जीवित या किसी एक समय पर जीवित सामग्री) से कम समय (दिन, सप्ताह या महीनों) में उत्पन्न होता है, उसे जैव ईंधन माना जाता है। लोग वाहनों के लिए नेचुरल गैस और फ्यूल की उच्च कीमतों का पेमेंट कर रहे हैं, आने वाले सालों में इन दोनों की कीमत और बढ़ेगी जो हमारे बजट को नुकसान पहुंचाएगी और इससे बचने का कोई दूसरा तरीका नहीं है या फिर लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करें. जिससे वे ईंधनों में पैसा वेस्ट करने से बच सकते हैं. लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन हर कोई अफॉर्ड नहीं कर सकता है. इसलिए जैव इंधन का महत्व बढ़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है. यह ईंधन की कीमतों की तुलना में सस्ते हैं और ऊर्जा के बहुत अच्छे सोर्स हैं. जो प्रदूषण भी फैलाते नहीं है. इसलिए इस दिन को इसके महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है।
विश्व जैव ईंधन दिवस 2025 की थीम
विश्व जैव ईंधन दिवस 2025 की थीम है “जैव ईंधन: नेट ज़ीरो के लिए एक सतत मार्ग”. इस थीम का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करके शुद्ध-शून्य कार्बन भविष्य प्राप्त करने में जैव ईंधन की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालना है. यह थीम जैव ईंधन के महत्व को उजागर करती है, जो न केवल ऊर्जा सुरक्षा में योगदान करते हैं, बल्कि जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
जैव ईंधन के लाभ
* ये ऊर्जा के नवीकरणीय और जैव निम्नीकरणीय स्रोत हैं। जैसे- इथेनॉल, बायोडीज़ल, ग्रीन डीज़ल और बायोगैस आदि।
* जैव ईंधन, किसी भी प्रकार की जैविक सामग्री जैसे कृषि अपशिष्ट, या पेड़ और फसलों सहित वनस्पति से उत्पन्न हो सकता है।
* जैव ईंधन नवीकरणीय संसाधनों से बना है और जीवाश्म डीजल की तुलना में अपेक्षाकृत कम ज्वलनशील है. इसमें काफी बेहतर चिकनाई गुण होते हैं।
* यह मानक डीजल की तुलना में कम हानिकारक कार्बन उत्सर्जन का कारण बनता है।
*.कोयले और तेल के जलने से तापमान में वृद्धि होती है और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है. इसके विपरीत जैव ईंधन ग्रीनहाउस गैसों के प्रभाव को कम करते हैं।
* इसके उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण से मुक्ति मिलती है।
* जैव ईंधन कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करने और स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा देने में मदद करता है।
* यह ग्रामीण क्षेत्रों के लिये अतिरिक्त आय और रोज़गार सृजन में भी मदद करेगा।
* यह न केवल भारत की ग्रामीण ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करेगा, बल्कि परिवहन की बढ़ती मांगों को भी पूरा करेगा।
* जैव ईंधन के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और 21वीं सदी की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा।
आयोजन
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 से इसका आयोजन किया जा रहा है।
इंटरेस्ट सबवेंशन योजना
* यह अपशिष्ट से ऊर्जा संबंधी बायोमेथेनेशन परियोजनाओं और अभिनव व्यापार मॉडल के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
* औद्योगिक जैविक अपशिष्ट-से-ऊर्जा जैव-मीथेनेशन परियोजनाएँ आमतौर पर पूंजी गहन और वित्तीय रूप से परिचालन लागतों (जैसे- अपशिष्ट उपलब्धता) एवं राजस्व, विशेष रूप से बायोगैस यील्ड तथा इसके उपयोग, दोनों के प्रति ही संवेदनशील होती हैं।
* ऐसी परियोजनाओं में नवाचार का उद्देश्य समग्र ऊर्जा उत्पादन में सुधार करना होता है, जिससे ऊर्जा उत्पादन की लागत को कम-से-कम किया जा सके, लेकिन स्थापना चरण में प्रारंभिक परियोजना लागत अधिक हो सकती है फिर भी राजस्व में वृद्धि एवं परियोजना के जीवनकाल में परिचालन लागत कम होती है।
* यह ऋण योजना लाभार्थियों को ऐसी परियोजनाओं के सामने आने वाले ऋण घटक पर ब्याज़ के वित्तीय बोझ को कम करने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
जैविक अपशिष्ट स्ट्रीम्स का GIS आधारित इन्वेंटरी टूल
* यह टूल पूरे भारत में उपलब्ध शहरी और औद्योगिक जैविक कचरे एवं उनकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता के ज़िला स्तर का अनुमान प्रदान करता है।
* GIS (भौगोलिक सूचना प्रणाली) टूल SMEs (लघु एवं मध्यम उद्यम) और परियोजना डेवलपर्स को ऊर्जा परियोजनाओं के लिये नए अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजना स्थापित करने में सक्षम बनाएगा और देश में अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में बायोमेथेनेशन के तीव्र विकास की सुविधा प्रदान कर सकता है।
बायोमेथेनेशन
बायोमेथेनेशन का आशय ऐसी प्रकिया से है जिसके द्वारा कार्बनिक पदार्थों को अवायवीय परिस्थितियों में सूक्ष्मजैविक रूप से बायोगैस में परिवर्तित किया जाता है।
* इसमें सूक्ष्मजीवों के तीन मुख्य शारीरिक समूह शामिल हैं: किण्वन बैक्टीरिया, कार्बनिक अम्ल ऑक्सीकरण बैक्टीरिया और मिथेनोजेनिक आर्किया।
* सूक्ष्मजीव, जैव रासायनिक रूपांतरणों के कैस्केड के माध्यम से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक पदार्थों में विघटित कर देते हैं।
जैव ईंधन को बढ़ावा देने हेतु सरकार की पहल
जैव ईंधन का सम्मिश्रण : जैव ईंधन के सम्मिश्रण को बढ़ावा देने के लिये इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम, इथेनॉल के लिये प्रशासनिक मूल्य तंत्र,तेल विपणन कंपनियों (OMC) के लिये खरीद प्रक्रिया को सरल बनाना, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के प्रावधानों में संशोधन आदि कुछ पहलें की गई हैं।इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी (ICGEB) के शोधकर्त्ता जैव ईंधन उत्पादन के लिये साइनोबैक्टीरियम (Cyanobacterium) का उपयोग करने हेतु एक विधि विकसित कर रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने भी अधिशेष चावल को इथेनॉल में बदलने की अनुमति दी है।
प्रधानमंत्री जी-वन योजना, 2019 : इस योजना का उद्देश्य दूसरी पीढ़ी (2G) के इथेनॉल उत्पादन हेतु वाणिज्यिक परियोजनाओं की स्थापना के लिये एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना और इस क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा देना है।
गोबर-धन योजना: यह खेतों में मवेशियों के गोबर और ठोस कचरे को उपयोगी खाद, बायोगैस और बायो-सीएनजी में बदलने और इस प्रकार गाँवों को साफ रखने व ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने पर केंद्रित है।
रिपर्पज़ यूज़्ड कुकिंग ऑयल : इसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा लॉन्च किया गया था तथा इसका उद्देश्य एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र विकसित करना है जो प्रयुक्त कुकिंग आयल को बायो-डीज़ल में संग्रह व रूपांतरण करने में सक्षम हो।
जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2018 : इस नीति द्वारा गन्ने का रस, चीनी युक्त सामग्री जैसे- चुकंदर, मीठा शर्बत सोरघम, स्टार्च युक्त सामग्री तथा मानव उपभोग हेतु अनुपयुक्त क्षतिग्रस्त अनाज, जैसे- गेहूँ, टूटे चावल और सड़े हुए आलू का उपयोग करके एथेनॉल उत्पादन हेतु कच्चे माल के दायरे का विस्तार किया गया है।
आगे की राह
* भारत जैसे देश में परिवहन में जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने से कच्चे तेल के आयात बिल को कम करने में मदद मिलेगी।
* एक बड़ी कृषि अर्थव्यवस्था बनने हेतु भारत के पास बड़ी मात्रा में कृषि अवशेष उपलब्ध हैं, इसलिये देश में जैव ईंधन के उत्पादन की गुंजाइश बहुत अधिक है। जैव ईंधन नई नकदी फसलों के रूप में ग्रामीण और कृषि विकास में मदद कर सकता है।
* शहरों में उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट और नगरपालिका कचरे का उपयोग सुनिश्चित कर स्थायी जैव ईंधन उत्पादन के प्रयास किये जाने चाहिये। एक अच्छी तरह से डिज़ाइन और कार्यान्वित जैव ईंधन नीति भोजन एवं ऊर्जा दोनों प्रदान कर सकती है।
*.एक समुदाय आधारित बायोडीज़ल वितरण कार्यक्रम जो स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को लाभ पहुँचाता है, फीडस्टॉक को विकसित करने वाले किसानों से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक ईंधन का उत्पादन और वितरण करने वाला एक स्वागत योग्य कदम होगा।
विश्व जैव ईंधन दिवस भारत सरकार के लिए गैर-जीवाश्म ईंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक मंच है। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 हमें यह याद दिलाता है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना और सतत विकास की दिशा में कदम बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है. हमें अपने पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करनी चाहिए और जैव विविधता के संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास करने चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और संतुलित पर्यावरण सुनिश्चित किया जा सके. यह दिन देश में जैव ईंधन क्षेत्र को विकसित और मजबूत करने में सरकार की गतिविधियों का भी जश्न मनाता है।