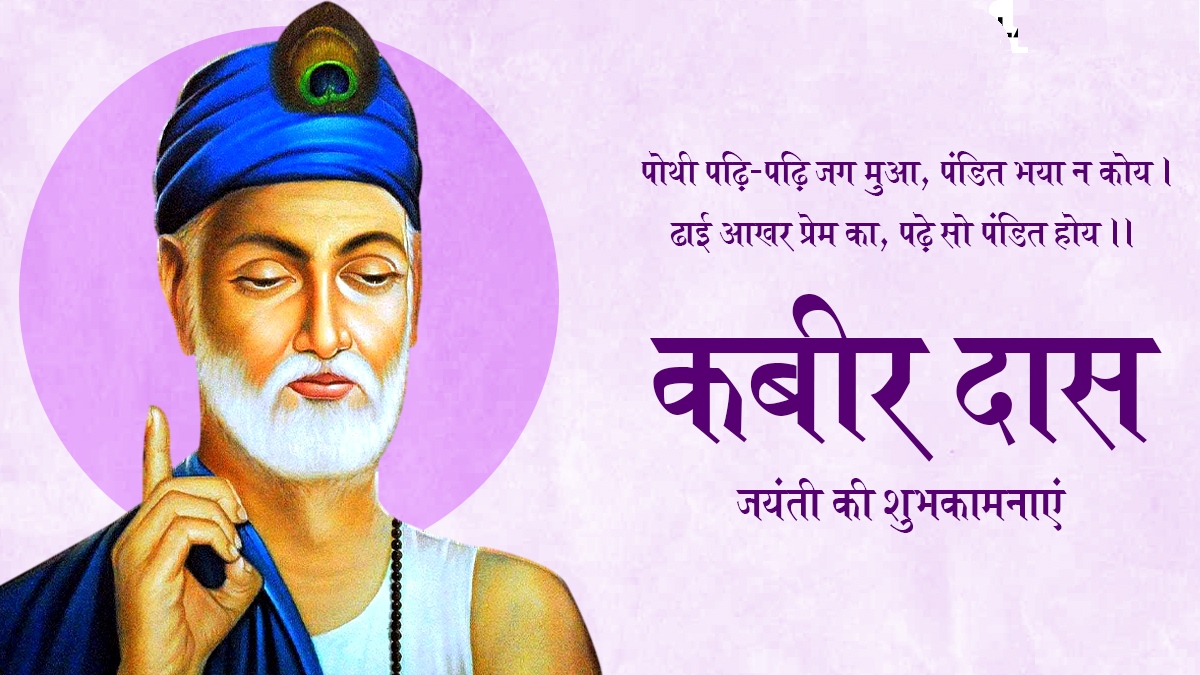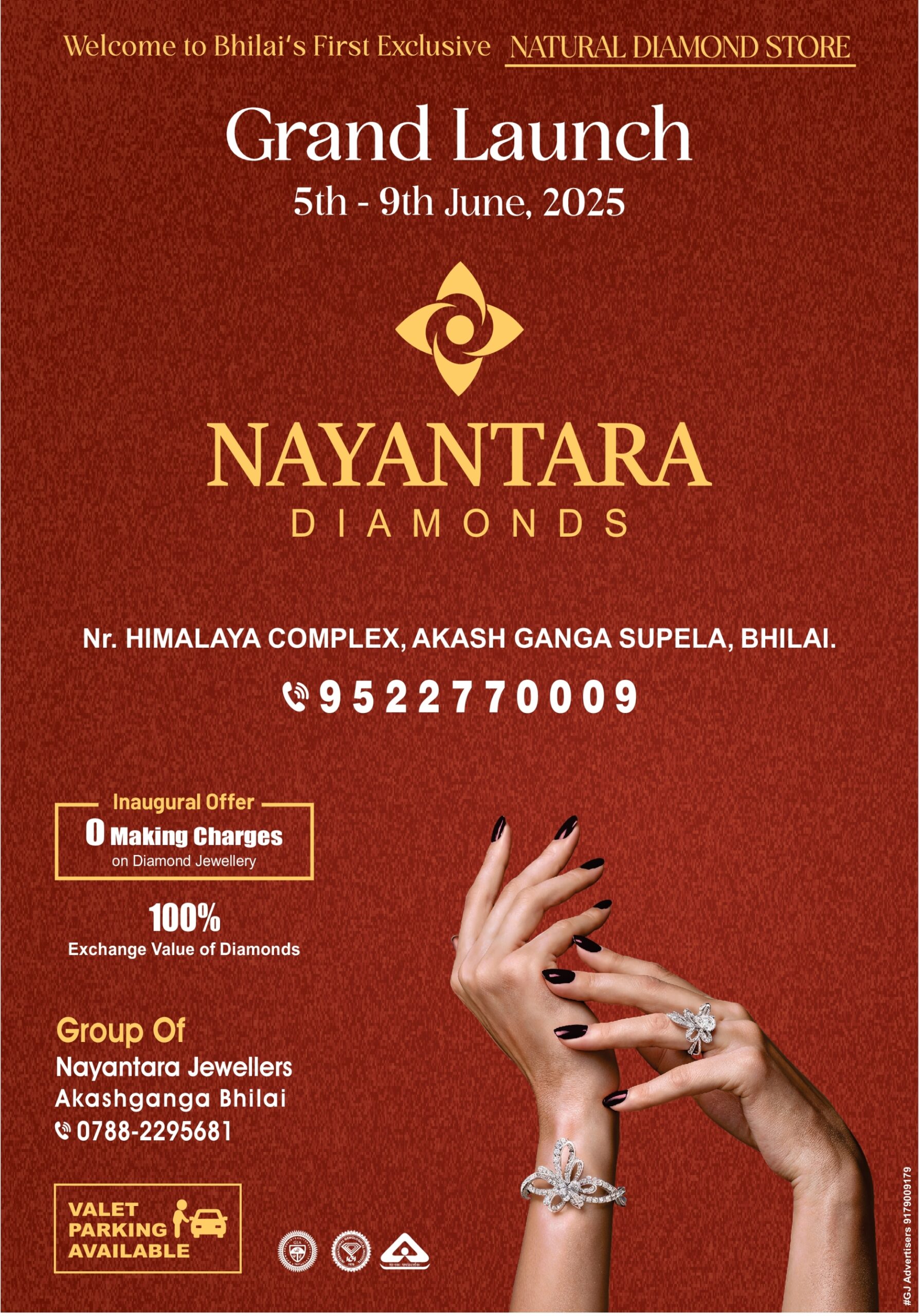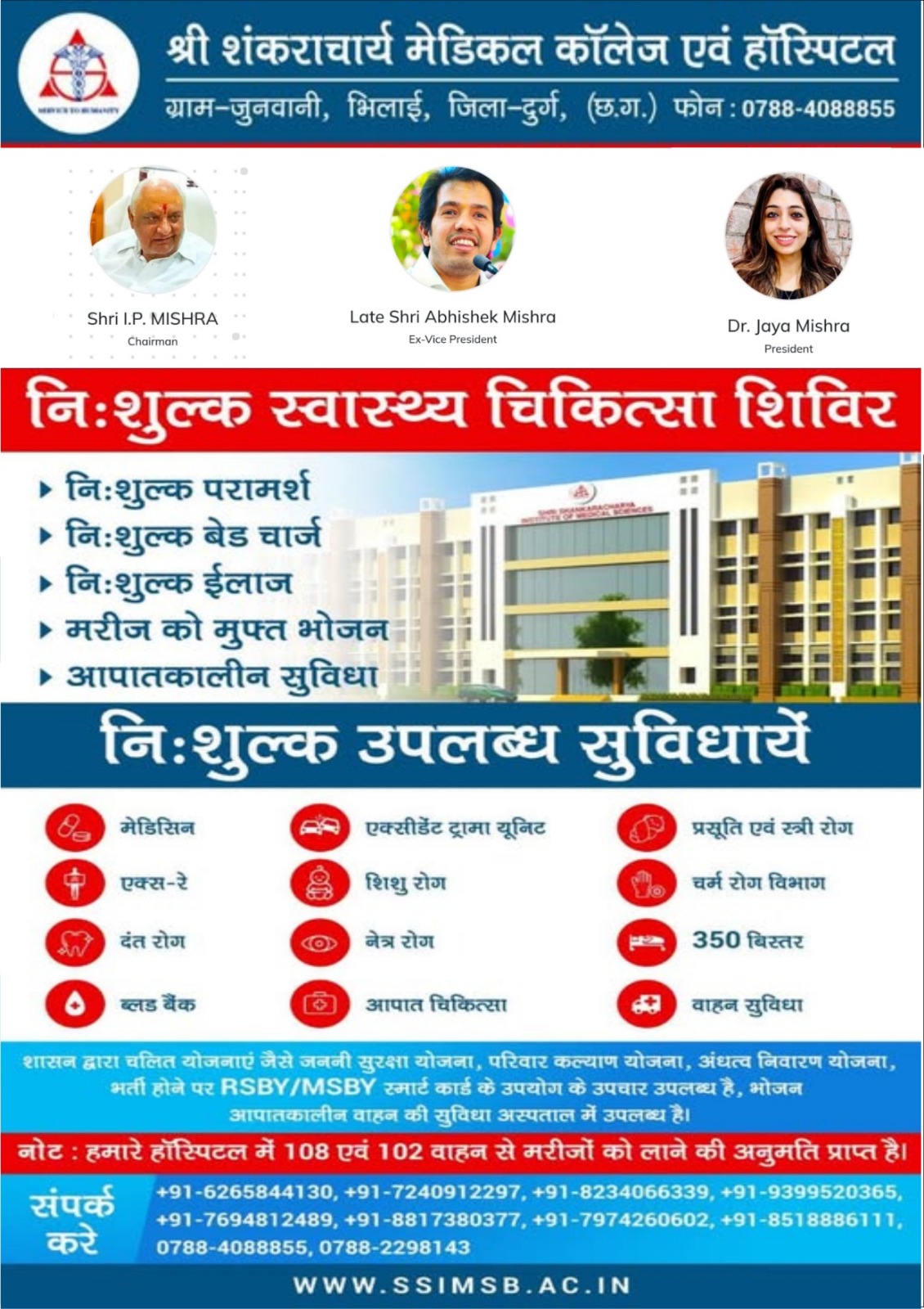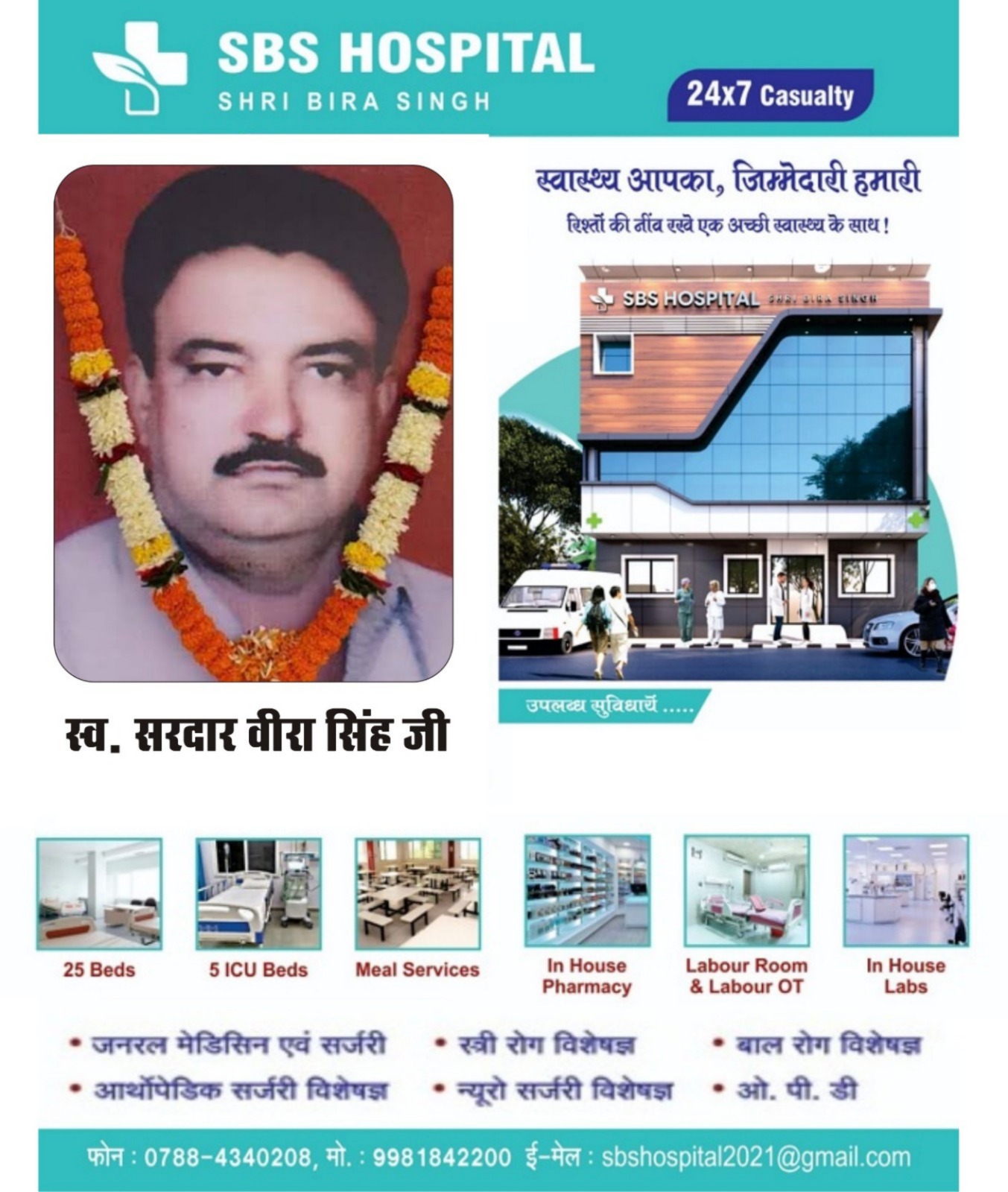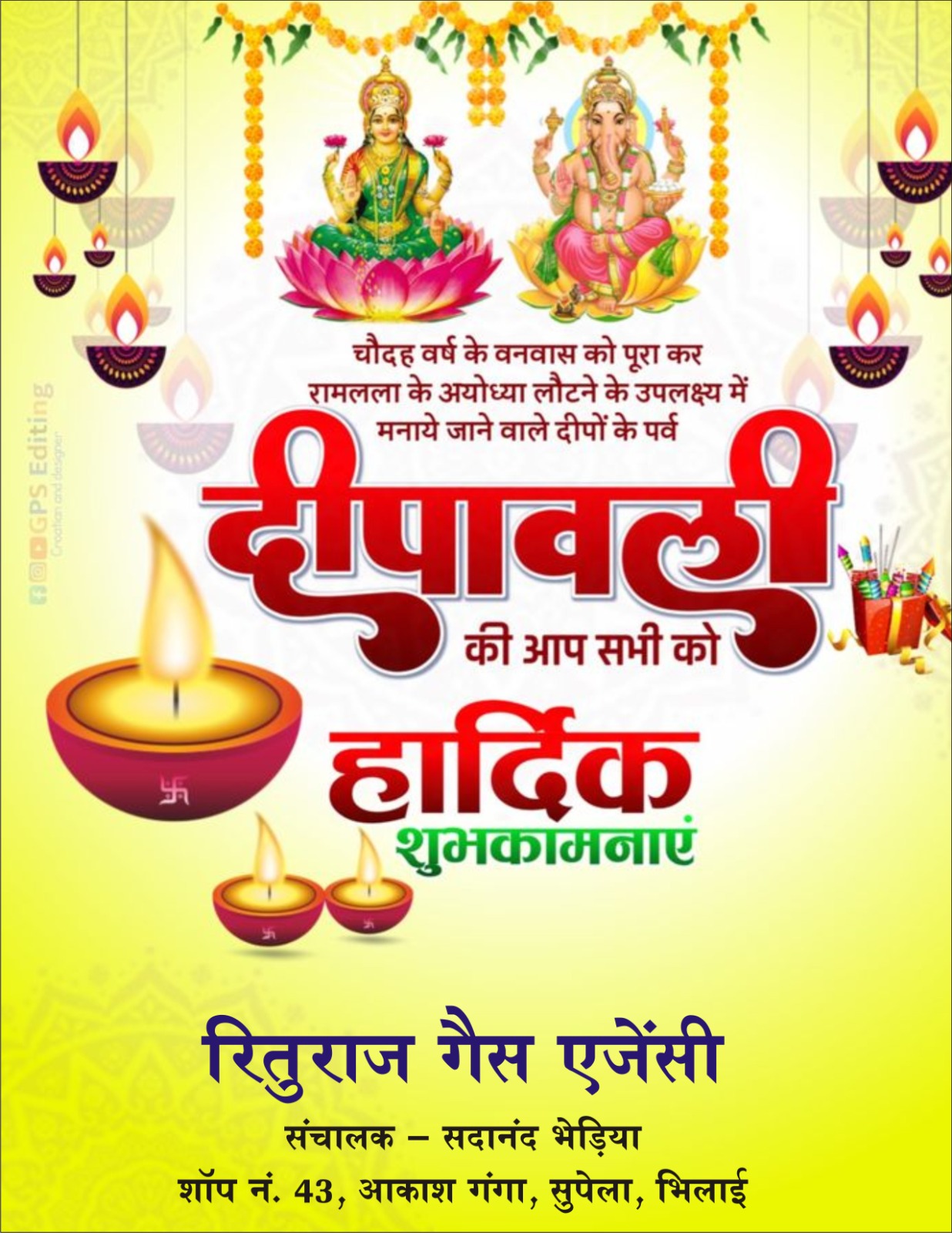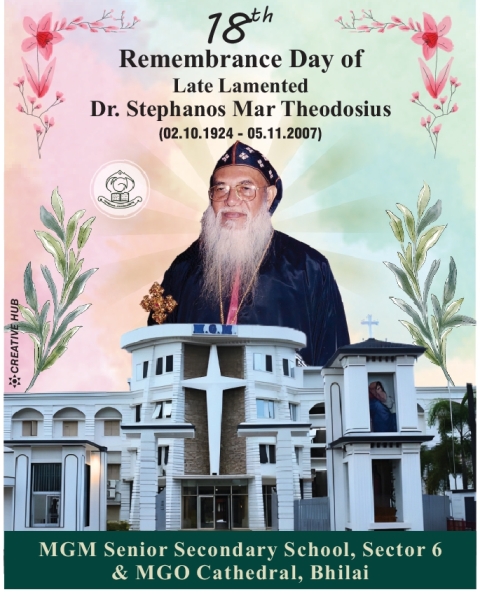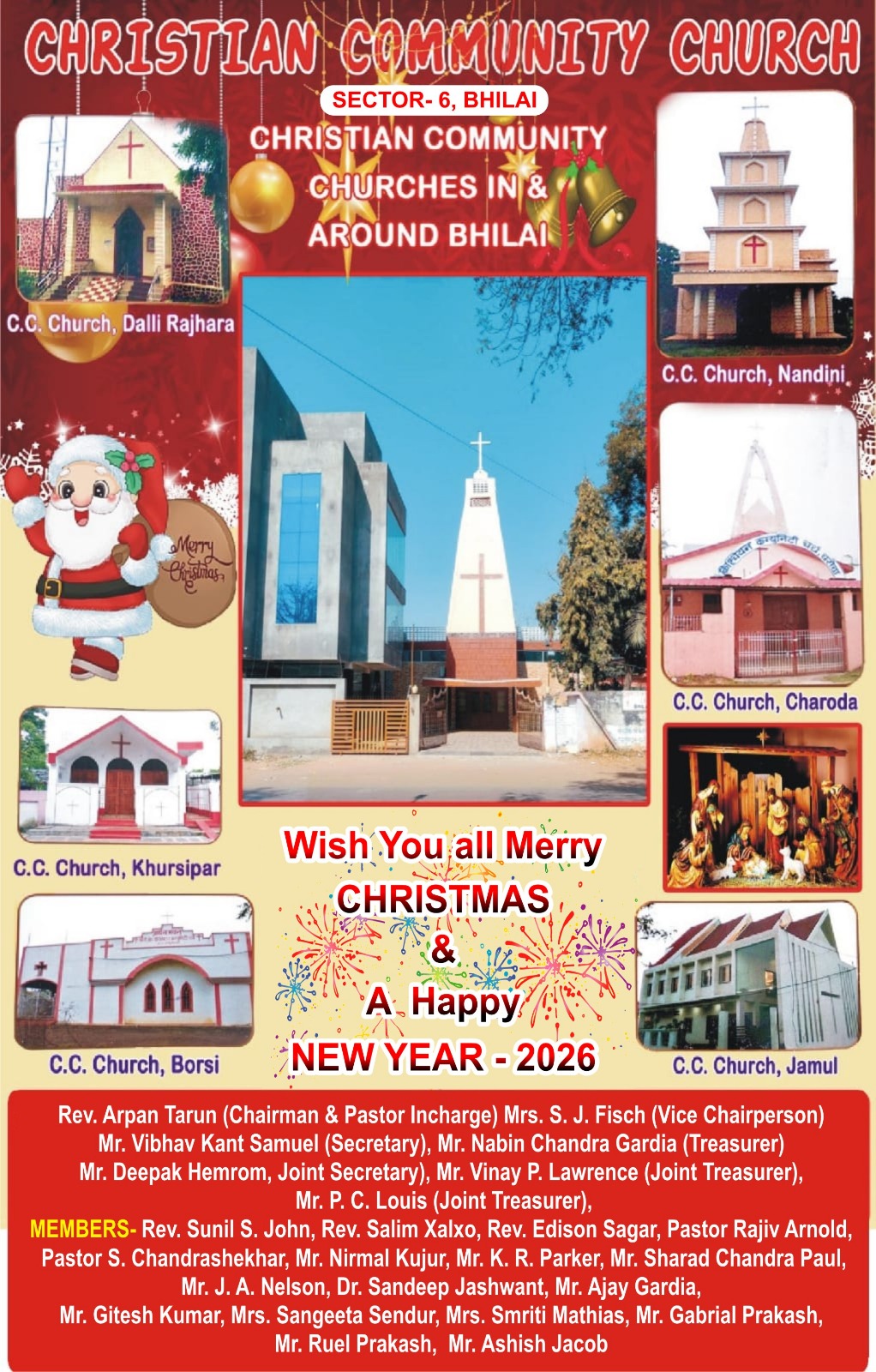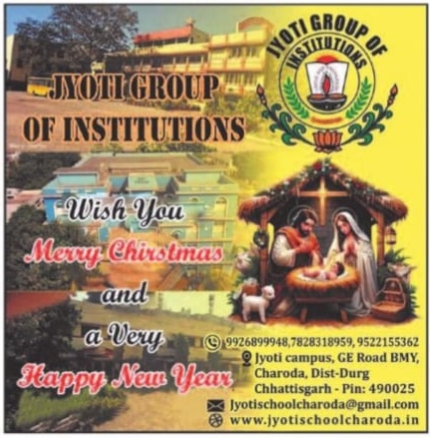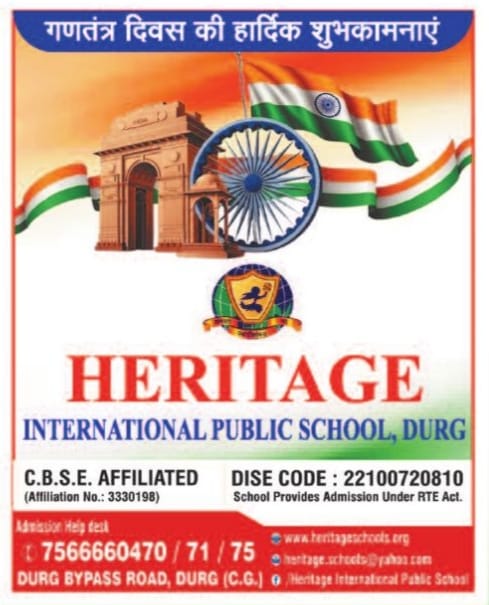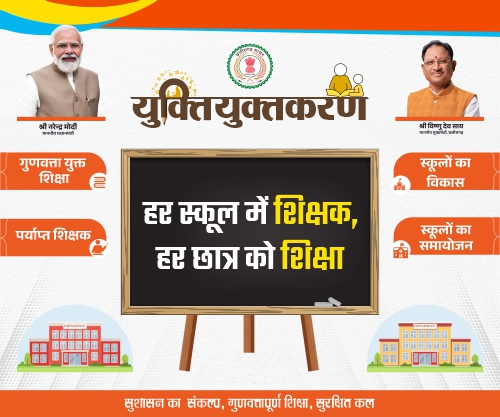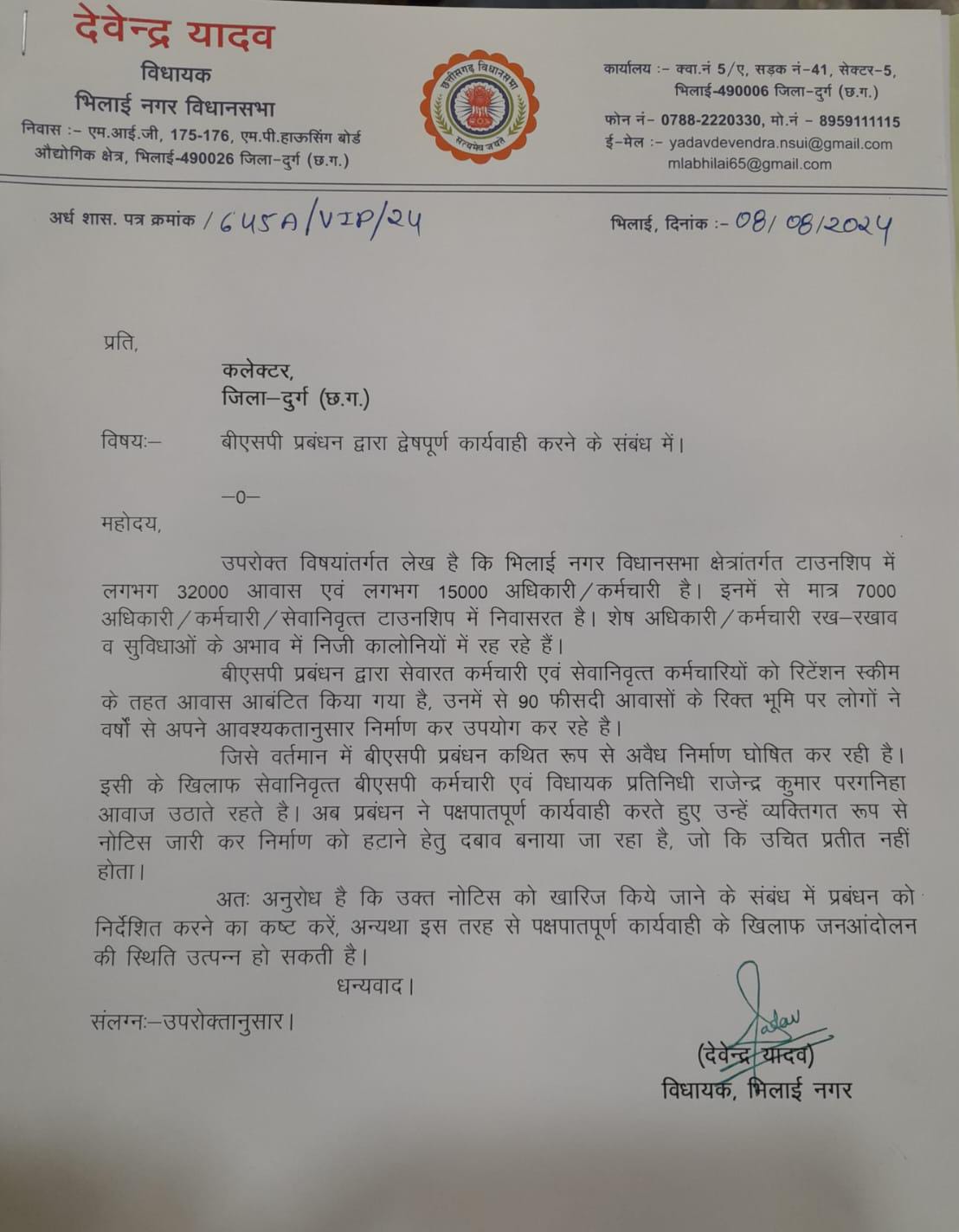संत कबीर दास 15वीं सदी में हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के सबसे प्रसिद्ध कवि, विचारक माने जाते हैं। इनका संबंध भक्तिकाल की निर्गुण शाखा “ज्ञानमर्गी उपशाखा” से था। इनकी रचनाओं और गंभीर विचारों ने भक्तिकाल आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया था। इसके साथ ही उन्होंने उस समय समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की। संत कबीर दास की रचनाओं के कुछ अंश सिक्खों के “आदि ग्रंथ” में भी सम्मिलित किए गए हैं। आइए जानते हैं संत कबीर दास का जीवन परिचय कैसा रहा।
भारत के महान संत कबीर दास का जन्म ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसीलिए हर वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ही उनकी जयंती मनाई जाती है। इस दिवस कबीर पंथ के अनुयायी कबीर के दोहे पढ़ते है उनकी शिक्षा से सबक लेते हैं। लोग कथा सत्संग का आयोजन करते है। इस दिन लोग अक्सर उनके जन्म स्थान वाराणसी के कबीर चौथा मठ में धार्मिक उपदेश का आयोजन करते हैं। कई जगह तो कबीर दास जयंती के अवसर पर भव्य जश्न मनाया जाता है। जबकि कई जगहों पर धार्मिक जुलूस और शोभायात्रा भी निकाल जाती है।कबीरदास की जयंती न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। संत कबीरदास की जयंती प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। साल 2024 में संत कबीरदास जी की जयंती 22 जून 2024, दिन शनिवार को मनाई जायेगी। अपनी प्रभावशाली परंपराओं और संस्कृति के कारण उन्हें दुनिया भर में प्रसिद्धि मिली।दोस्तों ! इस लेख में हम आपको बताने वाले हैं महान संत कबीरदास के जीवन से जुड़ी ढेर सारी जानकारी तो दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं विस्तार से कबीरदास जी के बारे में…..
कबीरदास का जीवन परिचय
नाम : संत कबीर दास
अन्य नाम : कबीरदास, कबीर परमेश्वर, कबीर साहब, कबीरा
जन्म : सन् 1398 (विक्रम संवत 1455) लहरतारा, काशी, उत्तर प्रदेश
मृत्यु : सन् 1519 (विक्रम संवत 1575) मगहर, उत्तर प्रदेश (120 वर्ष)
नागरिकता : भारतीय
शिक्षा : निरक्षर (पढ़े-लिखे नहीं)
पेशा : संत (ज्ञानाश्रयी निर्गुण), कवि, समाज सुधारक, जुलाहा
पिता-माता : नीरू, नीमा
गुरु : रामानंद
मुख्य रचनाएं : सबद, रमैनी, बीजक, कबीर दोहावली, कबीर शब्दावली, अनुराग सागर, अमर मूलभाषाअवधी, साधुक्कड़ी, पंचमेल खिचड़ी
कबीरदास का जन्म और प्रारम्भिक जीवन
भारत के महान संत कबीर का जन्म सन 1398 ईसवी में एक जुलाहा परिवार में हुआ था उनके पिता का नाम नीरू एवं माता का नाम नीमा था। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि कबीर किसी विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे ,जिसने लोक लाज के डर से जन्म देते ही कबीर को त्याग दिया था। नीरू और नीमा को कबीर पड़े हुए मिले और उन्होंने कबीर का पालन-पोषण किया। कबीर के गुरु प्रसिद्ध संत स्वामी रामानंद थे। लोक कथाओं के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि कबीर विवाहित थे। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनकी दो संताने थी एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली।
कबीर दास की शिक्षा
कबीर ने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली और न ही उन्होंने कभी कागज़ कलम को छुआ। वे अपनी आजीविका के लिए जुलाहे का काम करते थे। कबीर अपनी आध्यात्मिक खोज को पूर्ण करने के लिए वाराणसी के प्रसिद्ध संत रामानंद के शिष्य बनना चाहते थे। स्वामी रामानन्द जी अपने समय के सुप्रसिद्ध ज्ञानी कहे जाते थे पर रामानंद उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते थे। किन्तु कबीर ने उन्हें मन ही मन अपना गुरु मान लिया था। वे अपने गुरु से गुरु मंत्र लेना चाहते थे पर कबीर दास को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। कबीर दास जब संत रामानंद रात्रि चार बजे स्नान के लिए काशी घाट पर जाते थे तो उनके मार्ग में लेट जाते थे ताकि उनके गुरु मुख से जो भी पहला शब्द निकले उसे ही गुरु मंत्र मान लेंगे। तब एक दिन मार्ग में उनके गुरु के पैर कबीर पर पड़े तो संत रामानंद ने अपने मुंह से “राम” नाम लिया। बस कबीर ने उसे ही गुरु मंत्र मान लिया। कुछ लोग मानते हैं कि कबीर दास जी के कोई गुरु नहीं थे। उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ वह अपनी ही बदौलत प्राप्त किया। वे पढ़े-लिखे नहीं थे यह बात उनके इस दोहा से मिलता है – कबीर दास जी ने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखा, उन्होंने सिर्फ उसे बोले थे। उनके शिष्यों ने उनके द्वारा कही गई बातों और उपदेशों को कलमबद्ध किया था। कबीर दास के बारे में जानकर ही आश्चर्य होता है कि उन्होंने कभी कागज कलम को हाथ तक नहीं लगाया, ना ही कोई पढ़ाई की और न ही उनके कोई औपचारिक गुरु थे। पर कैसे उन्हें इतना आत्मज्ञान प्राप्त हुआ? यह अपने आप में हैरान करने वाला है। कबीर दास के जीवन पर आज के पढ़े लिखे लोग पीएचडी कर रहे हैं।
कबीर दास की मृत्यु
15वीं शताब्दी के सूफी कवि कबीर दास के अनुसार, ऐसी मान्यता है कि उन्होंने अपनी मृत्यु का स्थान मगहर चुना था, जो लखनऊ से लगभग 240 किमी दूर स्थित है। उन्होंने लोगों के मन से परियों की कहानी (मिथक) को दूर करने के लिए इस जगह को मरने के लिए चुना है। उन दिनों यह माना जाता था कि जो व्यक्ति मगहर क्षेत्र में अपनी अंतिम सांस लेते है और मर जाते है, उसे स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी और साथ ही अगले जन्म में गधे का जन्म भी नहीं होगा। लोगों के मिथकों और अंधविश्वासों को तोड़ने के कारण कबीर दास की मृत्यु काशी के बजाय मगहर में हुई। विक्रम संवत 1575 में हिंदू कैलेंडर के अनुसार, उन्होंने माघ शुक्ल एकादशी पर वर्ष 1518 में जनवरी के महीने में मगहर में दुनिया को छोड़ दिया।यह भी माना जाता है कि जो काशी में मर जाता है, वह सीधे स्वर्ग जाता है इसलिए हिंदू लोग अपने अंतिम समय में काशी जाते हैं और मोक्ष प्राप्त करने के लिए मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं। मिथक को ध्वस्त करने के लिए कबीर दास की मृत्यु काशी से हुई थी। इससे जुड़ी एक प्रसिद्ध कहावत है “जो कबीरा काशी मुए तो रमे कौन निहोरा” यानी काशी में मरने से ही स्वर्ग जाने का आसान रास्ता है तो भगवान की पूजा करने की क्या जरूरत है। मगहर में कबीर दास की मजार और समाधि है। उनकी मृत्यु के बाद उनके हिंदू और मुस्लिम धर्म के अनुयायी उनके शरीर के अंतिम संस्कार के लिए लड़ते हैं। लेकिन जब वे शव से चादर निकालते हैं तो उन्हें केवल कुछ फूल मिलते हैं जिन्हें उन्होंने अपने रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार अंतिम संस्कार पूरा किया। समाधि से कुछ मीटर की दूरी पर एक गुफा है जो मृत्यु से पहले उनके ध्यान स्थान का संकेत देती है। कबीर शोध संस्थान नाम का एक ट्रस्ट चल रहा है जो कबीर दास के कार्यों पर शोध को बढ़ावा देने के लिए एक शोध फाउंडेशन के रूप में काम करता है। यहां शैक्षणिक संस्थान भी चल रहे हैं जिनमें कबीर दास की शिक्षाएं शामिल हैं।
कबीरदास के गुरु
संत कबीर ने काशी के प्रसिद्ध महात्मा रामानंद को अपना गुरु माना है। कहा जाता है, कि रामानंद जी ने नीच जाति का समझकर कबीर को अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया था, तब एक दिन कबीर गंगा तट पर जाकर सीढ़ियों पर लेट गये जहां रामानंद जी प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने जाया करते थे। अंधेरे में रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ा और उनके मुख से राम राम निकला तभी से कबीर ने रामानंद जी को अपना गुरु और राम नाम को गुरु मंत्र मान लिया। कुछ विद्वानों ने प्रसिद्ध सूफी फकीर शेखतकी को कबीर का गुरु माना है।
कबीरदास जी की भाषा व प्रमुख रचनाएँ
कबीर दास द्वारा लिखी गई पुस्तकें आम तौर पर दोहों और गीतों का संग्रह हैं। कुल कार्य बहत्तर हैं जिनमें कुछ महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कार्य रेख़्तास, कबीर बीजक, सुक्निधान, मंगल, वसंत, सबदास, सखियाँ और पवित्र आगम हैं। कबीर दास की लेखन शैली और भाषा बहुत ही सरल और सुंदर है। उन्होंने अपने दोहों को बहुत ही साहस और स्वाभाविक रूप से लिखा था जो अर्थ और महत्व से भरे हुए हैं। उन्होंने अपने दिल की गहराई से इन्हें लिखा है। उन्होंने अपने सरल दोहों और दोहों में समस्त विश्व के भाव को संकुचित कर दिया है। उनकी बातें तुलना और प्रेरणा से परे हैं।
कबीर दास की रचनाएं
कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं को बेहद सरल और आसान भाषा में लिखा है, उन्होंने अपनी रचनाओं में बड़ी बेबाकी से धर्म, संस्कृति, समाज एवं जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय रखी है। उनके काव्य में आत्मा और परमात्मा के संबंधों की भी स्पष्ट व्याख्या मिलती है उनकी प्रमुख रचनाएं हैं –
साखी, सबद, रमैनी, कबीर बीजक, सुखनिधन, रक्त, वसंत, होली अगम
इन रचनाओं में कबीर का बीजक ग्रंथ प्रमुख है। उनकी रचनाओं में वो जादू है जो किसी और संत में नहीं है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को “वाणी का डिक्टेटर” कहा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को ‘पंचमेल खिचड़ी’ कहा है।
कबीर का साहित्यिक परिचय
कबीर एक महान संत भी थे और संसारी भी, समाज सुधारक भी थे और एक सजग कवि भी। वह अनाथ थे, लेकिन सारा समाज उनकी छत्रछाया की अपेक्षा करता था। कबीर के महान व्यक्तित्व एवं उनके काव्य के संबंध में हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉ प्रभाकर माचवे ने लिखा है – “कबीर में सत्य कहने का अपार धैर्य था और उसके परिणाम सहन करने की हिम्मत भी। कबीर की कविता इन्हीं कारणों से एक अन्य प्रकार की कविता है। वह कई रूढ़ियों के बंधन तोड़ता है वह मुक्त आत्मा की कविता है।”
कबीरदास की रचनाएँ
आपको बता दे की संत कबीर पढ़े-लिखे नहीं थे उन्होंने स्वयं ही कहा है –
मसि कागद छुयो नहीं, कलम गह्यो नहीं हाथ।।अतः यह सत्य है कि उन्होंने स्वयं अपनी रचनाओं को नहीं लिखा है। इसके बाद भी उनकी वाणीयों के संग्रह के रूप में कई ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में- ‘अगाध-मंगल’, ‘अनुराग सागर’, ‘अमर मूल ‘, ‘अक्षर खंड रमैनी’, ‘अक्षर भेद की रमैनी’, ‘उग्र गीता’, ‘कबीर की वाणी’, ‘कबीर ‘, ‘कबीर गोरख की गोष्ठी’, ‘कबीर की साखी’, ‘बीजक’, ‘ब्रह्म निरूपण’, ‘मुहम्मद बोध’, ‘रेख़्ता विचार माला’, ‘विवेकसागर’, ‘शब्दावली ‘, ‘हंस मुक्तावली’, ‘ज्ञान सागर’ आदि प्रमुख ग्रंथ हैं इन ग्रंथों को पढ़ने से हमें कबीर की विलक्षण प्रतिभा का परिचय मिलता है। कबीर की वाणियों का संग्रह ‘बीजक’ के नाम से प्रचलित है इसके तीन भाग हैं –
(1) साखी
(2) सबद
(3) रमैनी
कबीर दास: एक हिंदू या एक मुसलमान
ऐसा माना जाता है कि कबीर दास की मृत्यु के बाद, हिंदुओं और मुसलमानों ने कबीर दास का शव प्राप्त करने का दावा किया था। वे दोनों कबीर दास के शव का अंतिम संस्कार अपने-अपने रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार करना चाहते थे।हिंदुओं ने कहा कि वे शरीर को जलाना चाहते हैं क्योंकि वह एक हिंदू थे और मुसलमानों ने कहा कि वे उसे मुस्लिम संस्कार के तहत दफनाना चाहते हैं क्योंकि वह एक मुसलमान थे। लेकिन, जब उन्होंने शव से चादर हटाई तो उन्हें उसके स्थान पर केवल कुछ फूल मिले। उन्होंने एक-दूसरे के बीच फूल बांटे और अपनी-अपनी परंपराओं और रीति-रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार किया। यह भी माना जाता है कि जब वे लड़ रहे थे तो कबीर दास की आत्मा उनके पास आई और उन्होंने कहा कि, “मैं न तो हिंदू था और न ही मुसलमान। मैं दोनों था, मैं कुछ भी नहीं था, मैं ही सब कुछ था, मैं दोनों में ईश्वर को पहचानता हूं। न कोई हिंदू है और न कोई मुसलमान। जो मोह से मुक्त है उसके लिए हिन्दू और मुसलमान एक ही हैं। कफन हटाओ और चमत्कार देखो!” कबीर दास का मंदिर काशी में कबीर चौरा पर बना है जो अब पूरे भारत के साथ-साथ भारत के बाहर लोगों के लिए महान तीर्थ स्थान बन गया है। और उसकी एक मस्जिद मुसलमानों द्वारा कब्र के ऊपर बनाई गई थी जो मुसलमानों के लिए तीर्थ बन गई है।
कबीर दास के ईश्वर के प्रति विचार
संतकबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है। जिस प्रकार विश्व में एक ही वायु और जल है, उसी प्रकार संपूर्ण संसार में एक ही परम ज्योति व्याप्त है। सभी मानव एक ही मिट्टी से अर्थात् ब्रम्ह द्वारा निर्मित हुए हैं। कबीर दास ने ईश्वर प्राप्ति के प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। कबीर के अनुसार ईश्वर न मंदिर में है, न मस्जिद में; न काबा में हैं, न कैलाश आदि तीर्थ स्थानों में; वह न योग साधना से मिलता है, और न वैरागी बनने से। ये सब उपरी दिखावे हैं, ढोंग हैं। इनसे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती।
कबीरदास के बारे में रोचक जानकारियाँ
1. कबीर मठ : कबीर मठ कबीर चौरा, वाराणसी और लहरतारा, वाराणसी में पीछे के मार्ग में स्थित है जहाँ संत कबीर के दोहे गाने में व्यस्त हैं। यह लोगों को जीवन की वास्तविक शिक्षा देने का स्थान है। नीरू टीला उनके माता-पिता नीरू और नीमा का घर था। अब यह कबीर के कार्यों का अध्ययन करने वाले छात्रों और विद्वानों के लिए आवास बन गया है।
2. दर्शन : कबीर दास पहले भारतीय संत हैं जिन्होंने हिंदू और इस्लाम दोनों को एक सार्वभौमिक मार्ग देकर हिंदू और इस्लाम का समन्वय किया है, जिसका पालन हिंदू और मुस्लिम दोनों कर सकते हैं। उनके अनुसार, प्रत्येक जीवन का दो आध्यात्मिक सिद्धांतों (जीवात्मा और परमात्मा) से संबंध है। मोक्ष के बारे में उनका विचार था कि यह इन दो दैवीय सिद्धांतों को एकजुट करने की प्रक्रिया है। उनकी महान कृति बीजक में कविताओं का एक विशाल संग्रह है जो कबीर के आध्यात्मिकता के सामान्य दृष्टिकोण को दर्शाता है। कबीर की हिन्दी एक बोली थी, उनके दर्शनों की तरह सरल। उन्होंने बस भगवान में एकता का पालन किया। उन्होंने हमेशा हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा को खारिज किया है और भक्ति और सूफी विचारों में स्पष्ट विश्वास दिखाया है।
3. उनकी कविता : उन्होंने एक वास्तविक गुरु की प्रशंसा के अनुरूप कविताओं की रचना एक संक्षिप्त और सरल शैली में की थी। अनपढ़ होने के बावजूद उन्होंने अवधी, ब्रज और भोजपुरी जैसी कुछ अन्य भाषाओं को मिलाकर हिंदी में अपनी कविताएँ लिखी थीं। हालाँकि कई लोगों ने उनका अपमान किया लेकिन उन्होंने कभी दूसरों पर ध्यान नहीं दिया।
4. विरासत : संत कबीर को श्रेय दी गई सभी कविताएँ और गीत कई भाषाओं में मौजूद हैं। कबीर और उनके अनुयायियों का नाम उनकी काव्य प्रतिक्रिया जैसे कि बनियों और कथनों के अनुसार रखा गया है। कविताओं को दोहे, श्लोक और सखी कहा जाता है। सखी का अर्थ है याद किया जाना और उच्चतम सत्य को याद दिलाना। इन कथनों को याद करना, प्रदर्शन करना और उन पर विचार करना कबीर और उनके सभी अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक जागृति का मार्ग है।
5. समाधि मंदिर : समाधि मंदिर का निर्माण उसी स्थान पर किया गया है जहाँ कबीर अपनी साधना करने के आदी थे। साधना से समाधि तक की यात्रा तब मानी जाती है जब कोई संत इस स्थान पर जाता है। आज भी यह वह स्थान है जहां संतों को अपार सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। यह जगह शांति और ऊर्जा के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ऐसा माना जाता है कि, उनकी मृत्यु के बाद, लोग उनके शरीर को अंतिम संस्कार के लिए लेने को लेकर झगड़ रहे थे। लेकिन, जब उनके समाधि कक्ष का दरवाजा खोला गया, तो केवल दो फूल थे, जो उनके हिंदू मुस्लिम शिष्यों के बीच अंतिम संस्कार के लिए वितरित किए गए थे। समाधि मंदिर का निर्माण मिर्जापुर की मजबूत ईंटों से किया गया है।
6. कबीर चबूतरा में बीजक मंदिर : यह स्थान कबीर दास का कार्यस्थल होने के साथ-साथ साधनास्थल भी था। यहीं पर उन्होंने अपने शिष्यों को भक्ति, ज्ञान, कर्म और मानवता का ज्ञान दिया था। इस जगह का नाम कबीर चबूतरा रखा गया। बीजक कबीर दास की महान कृति थी, इसलिए कबीर चबूतरा का नाम बीजक मंदिर पड़ा।
कबीर दास, भारत के प्रमुख आध्यात्मिक कवियों में से एक हैं जिन्होंने लोगों के जीवन को बढ़ावा देने के लिए अपने दार्शनिक विचार दिए हैं। ईश्वर में एकता के उनके दर्शन और वास्तविक धर्म के रूप में कर्म ने लोगों के मन को अच्छाई की ओर बदल दिया है। ईश्वर के प्रति उनका प्रेम और भक्ति हिंदू भक्ति और मुस्लिम सूफी दोनों की अवधारणा को पूरा करती है।
Disclaimer : इस पोस्ट में जो भी संत कबीरदास के जीवन से संबन्धित अभी तक जितने भी प्रमाण मिले हैं उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। स्वयं उनके द्वारा रचित काव्य और कुछ तत्कालीन कवियों द्वारा रचित काव्यों में उनके जीवन से संबन्धित तथ्य प्राप्त हुए हैं। इन तथ्यों के आधार पर इस पोस्ट में जानकारी दी है ”इस लेख में निहित किसी भी जानकारी/सामग्री/गणना में निहित सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारी आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना के तहत ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी।”