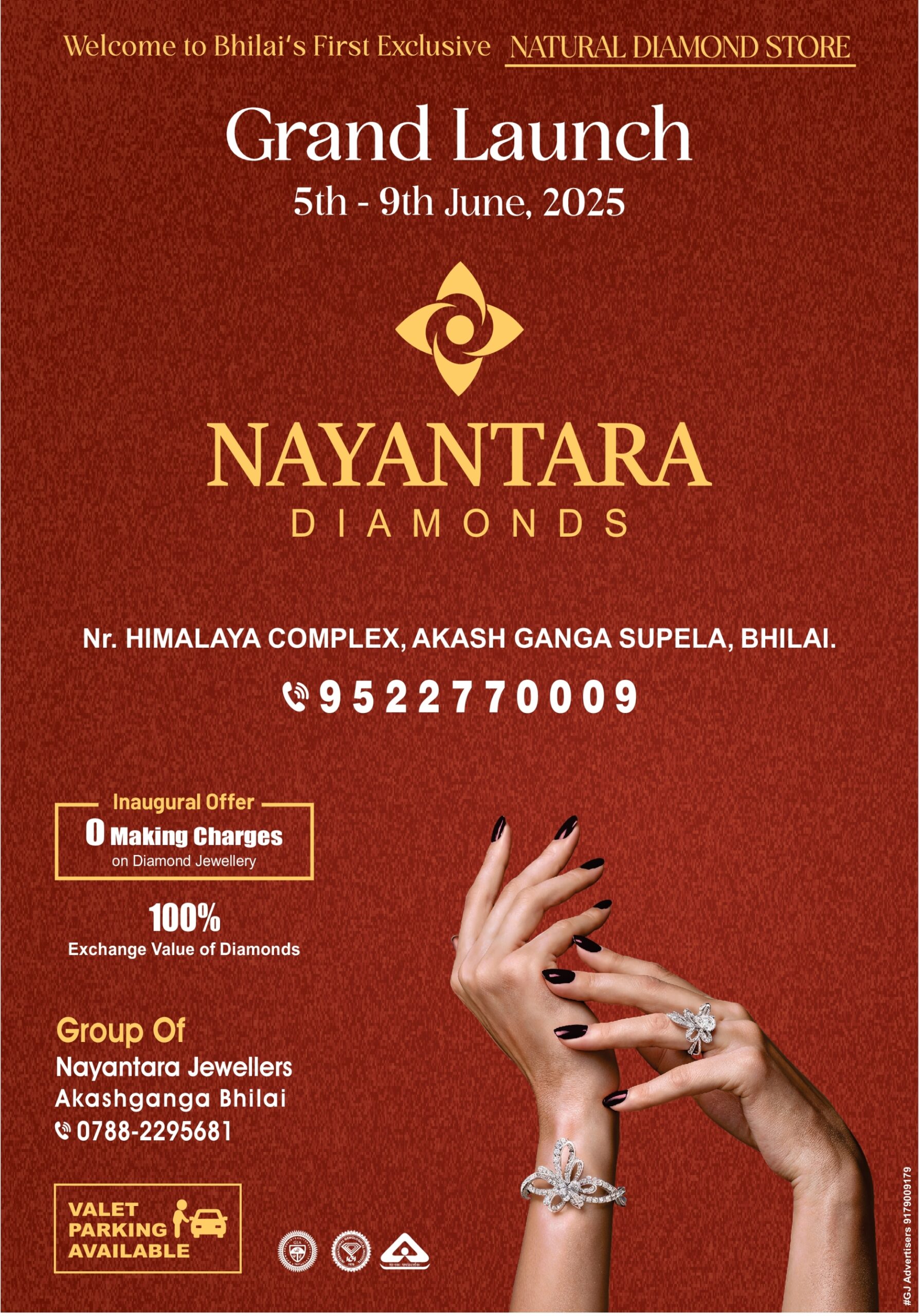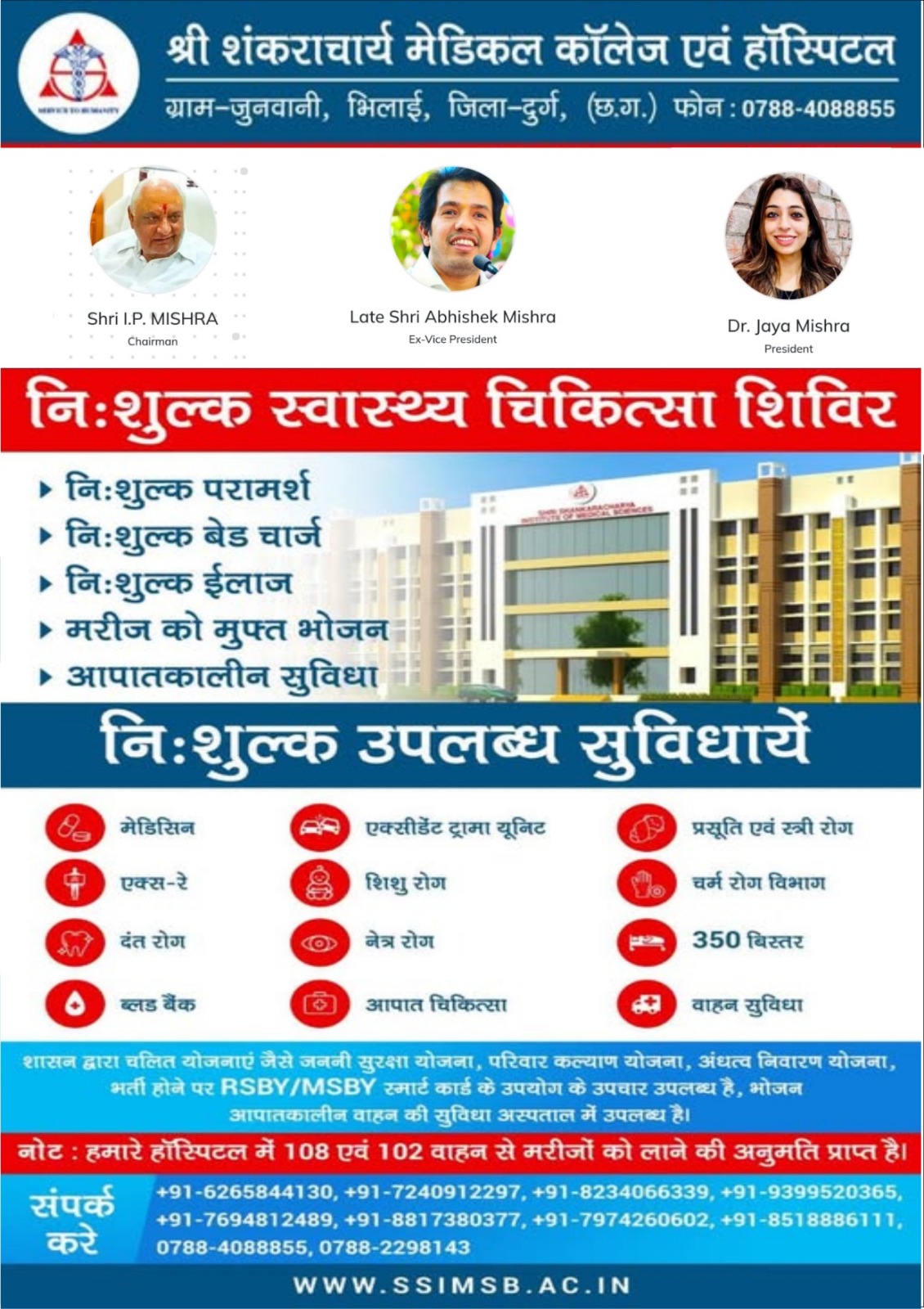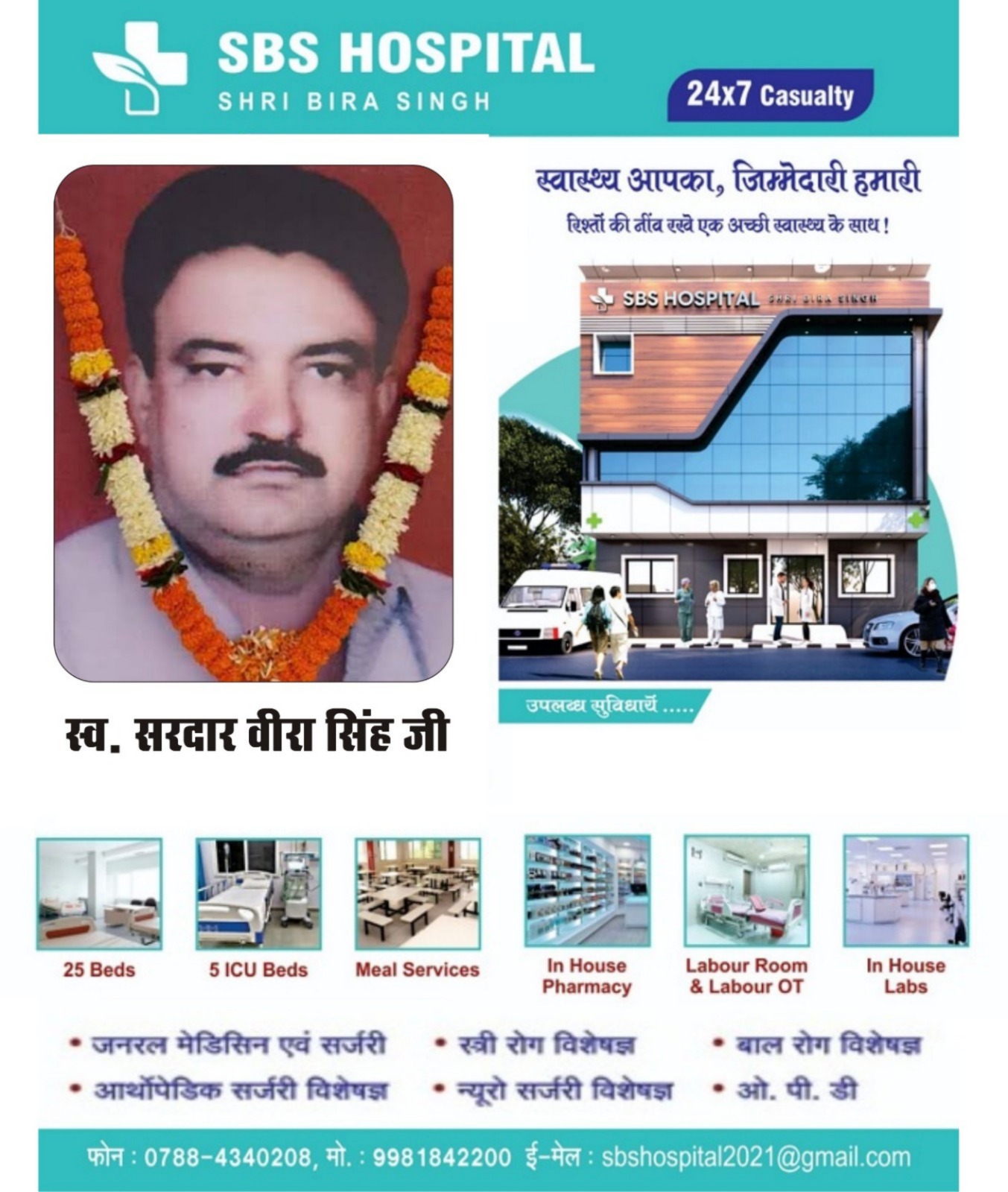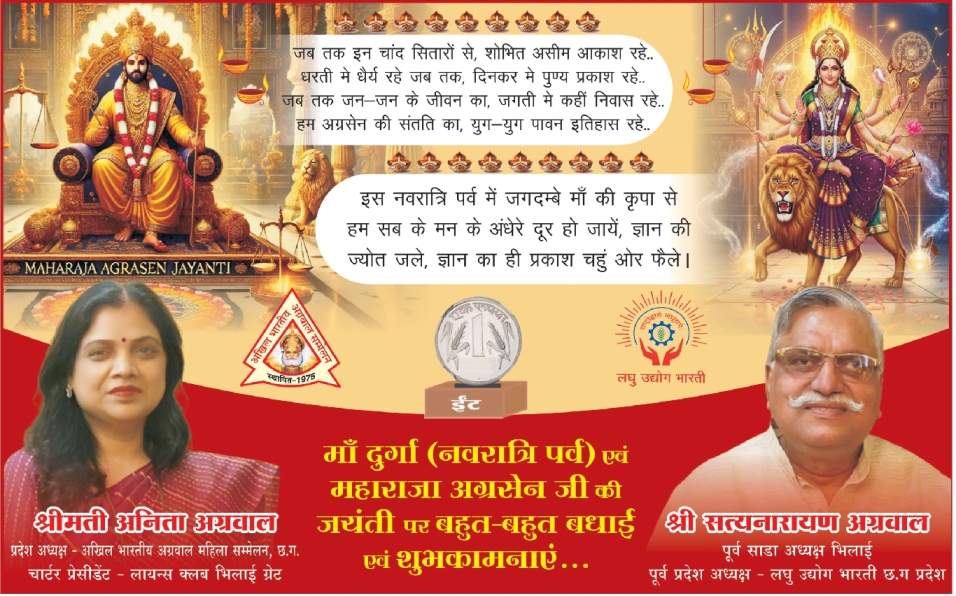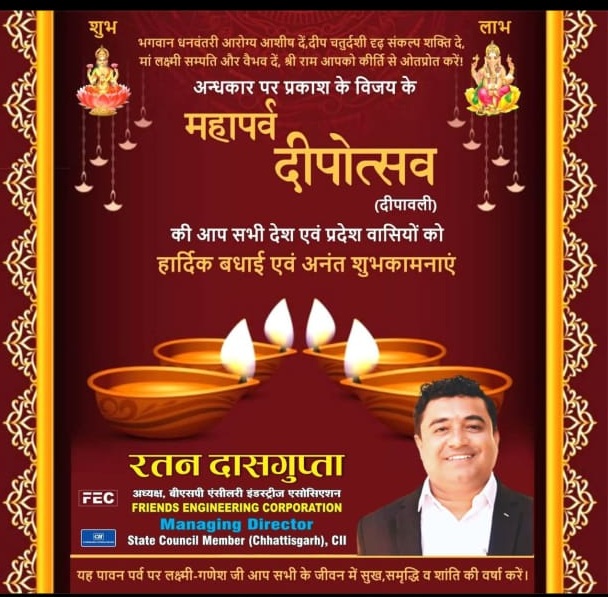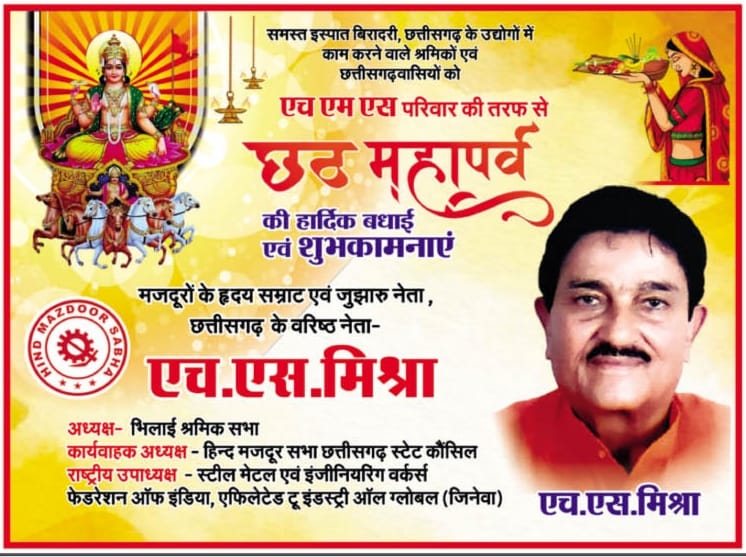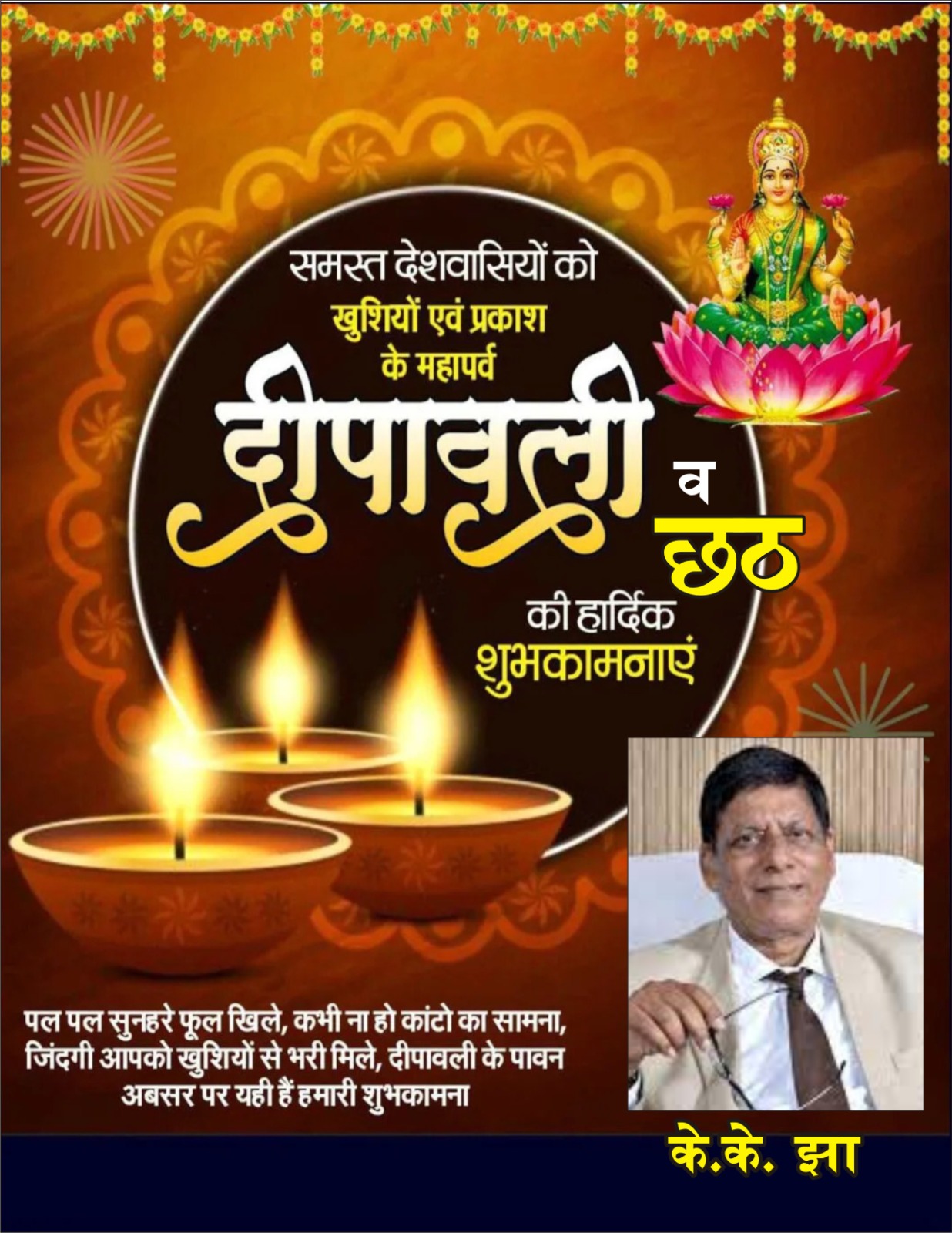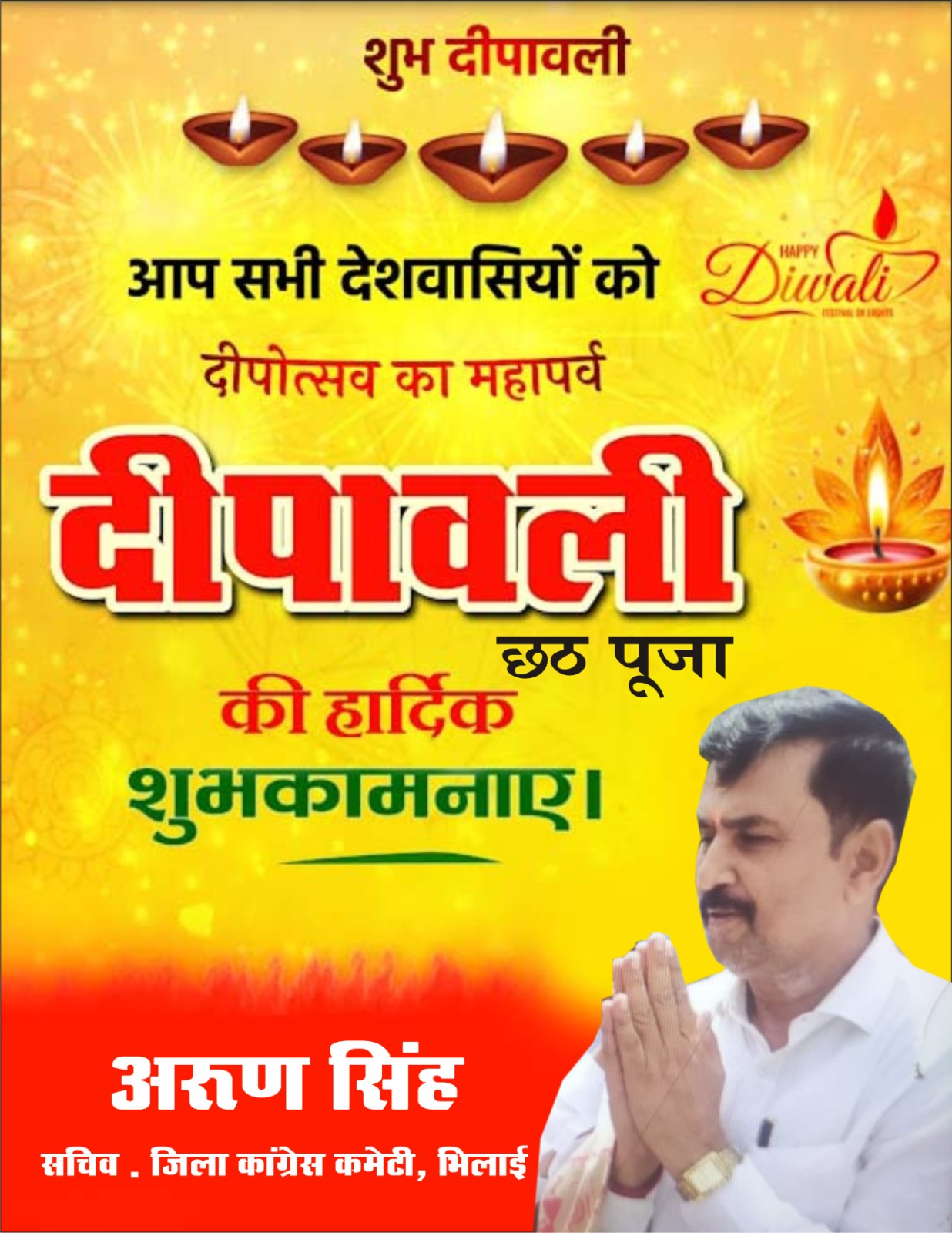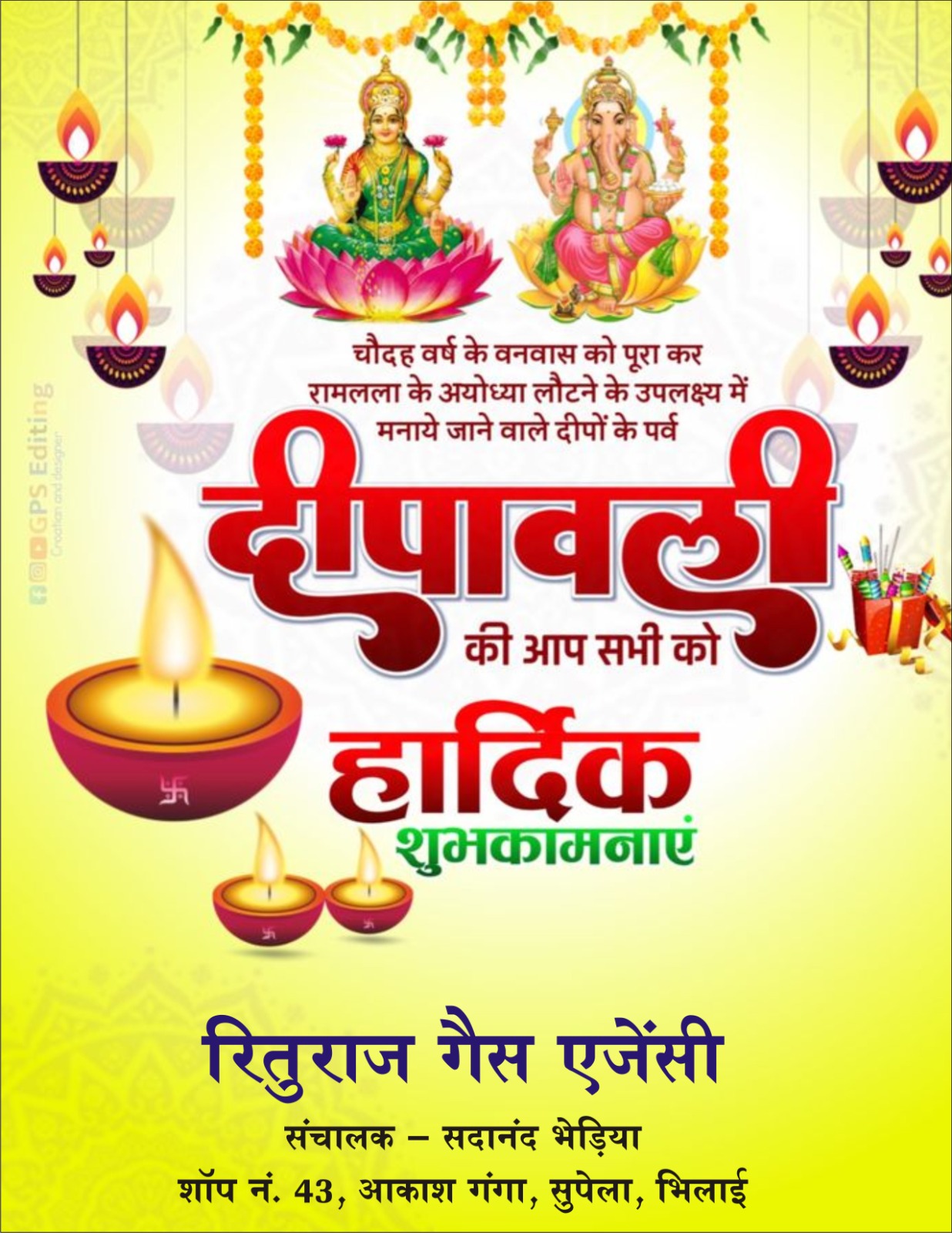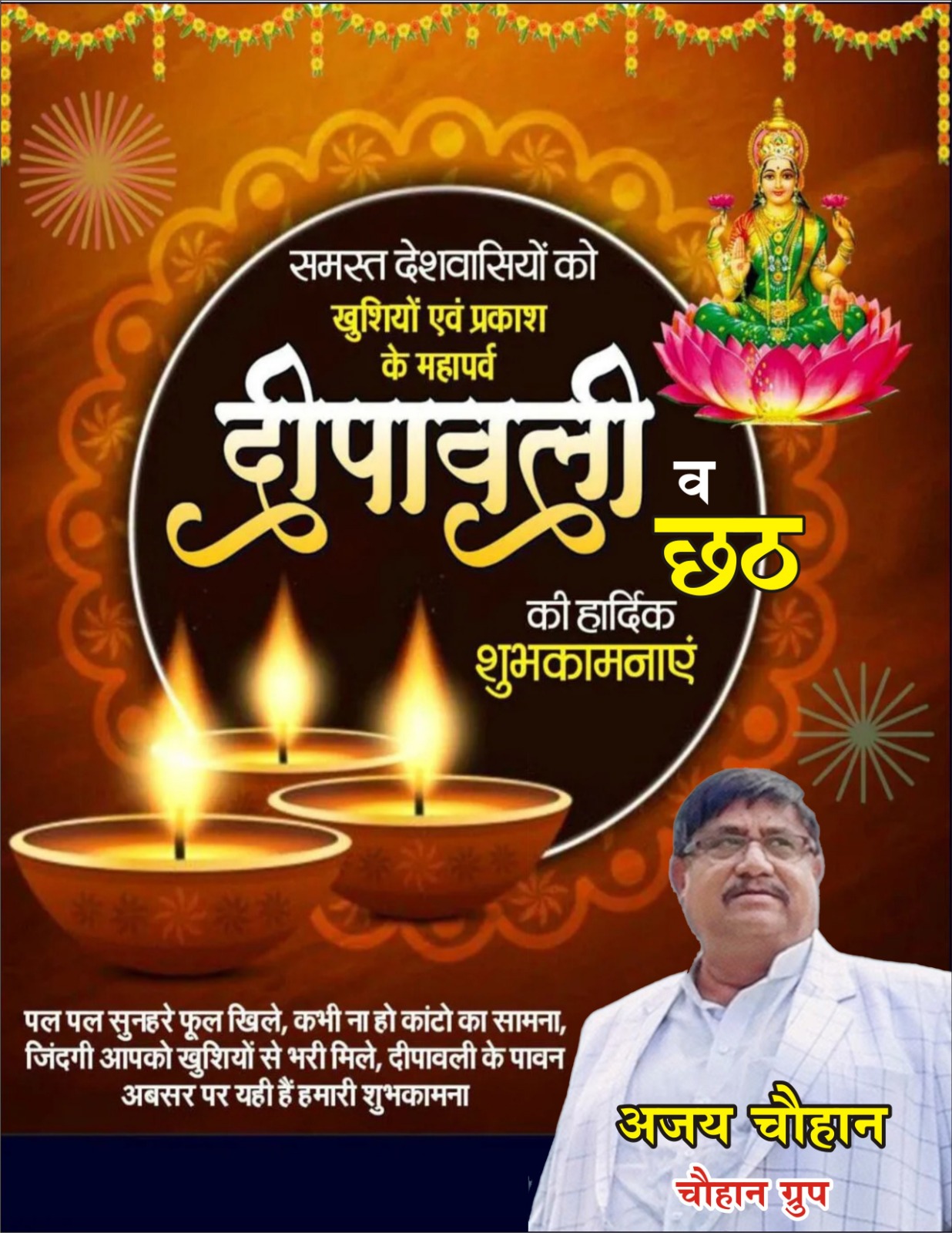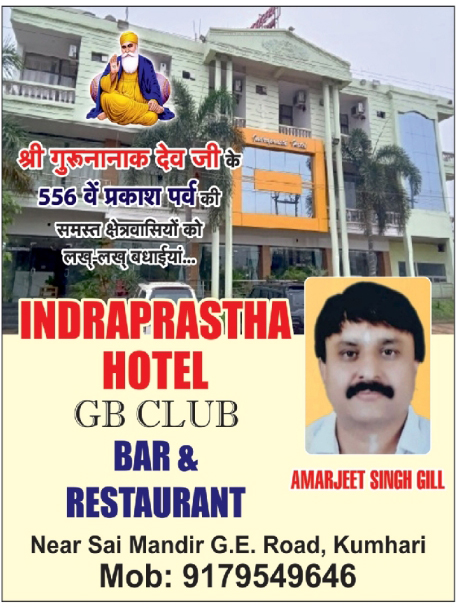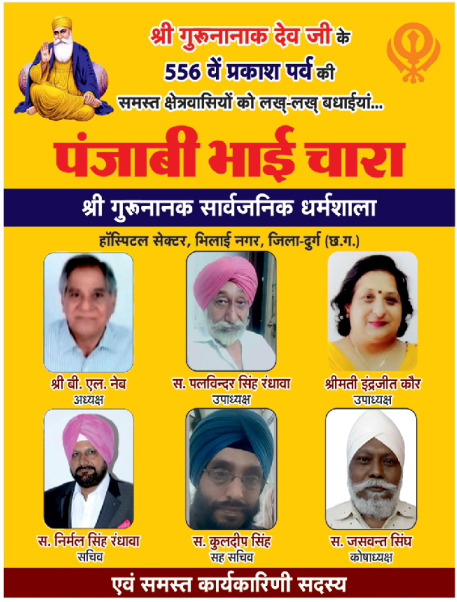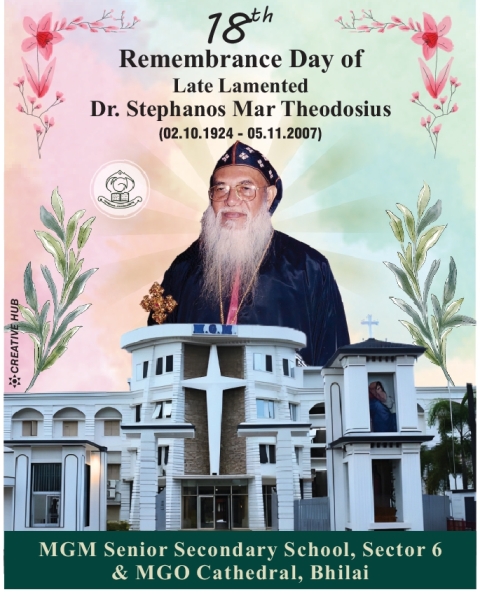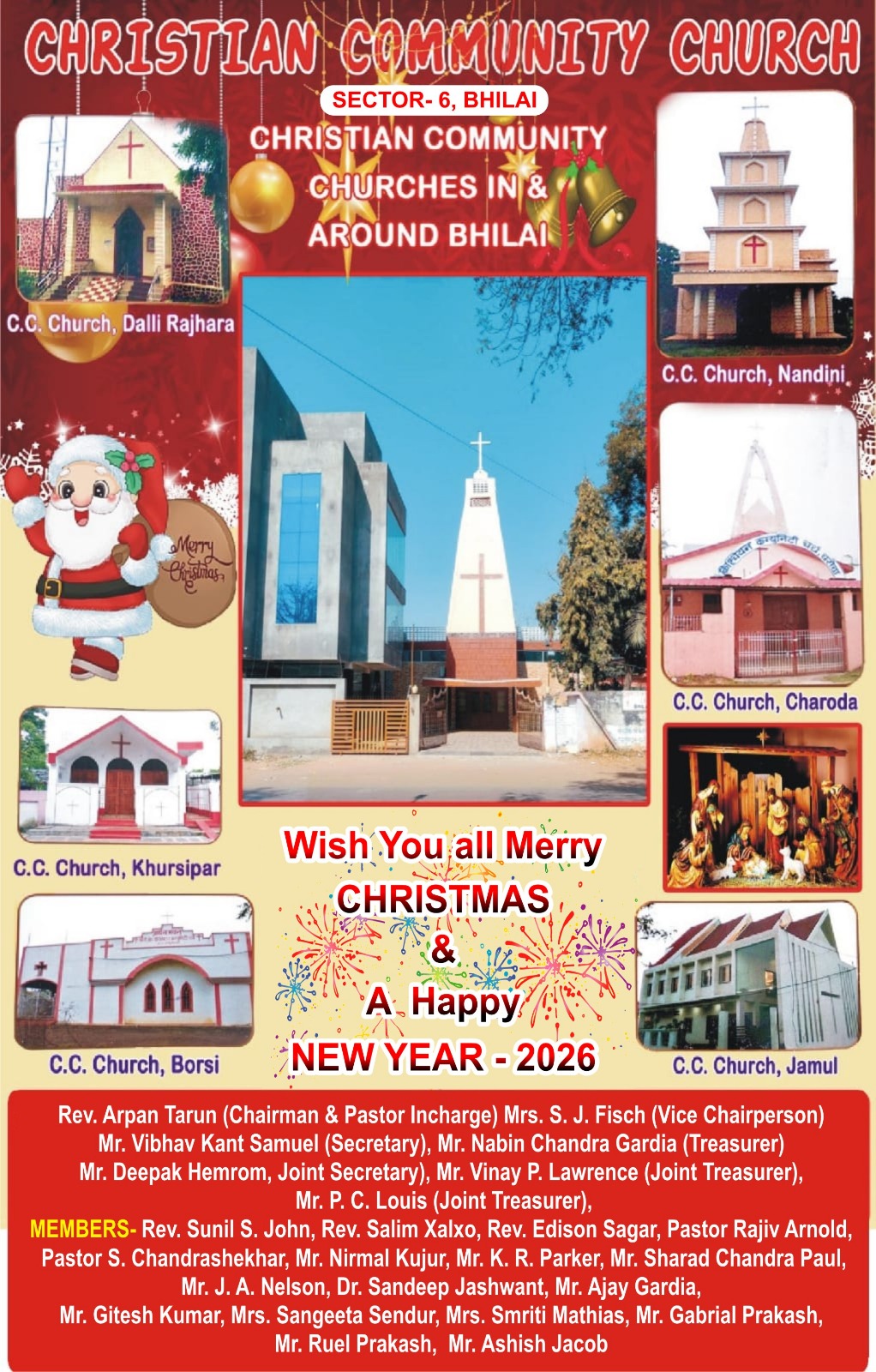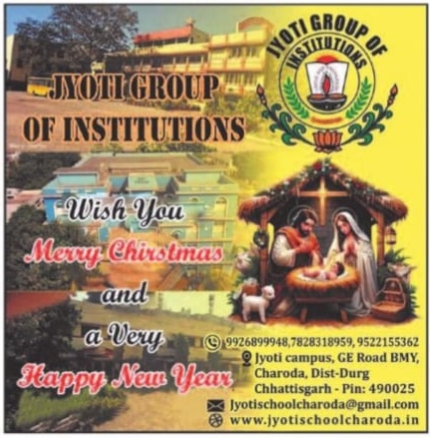वर्तमान समय में मानवीय अस्तित्व के लिए सबसे बड़े संकट की बात की जाए तो निःसंदेह ही पर्यावरण प्रदूषण धरती के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आज विश्व का प्रत्येक भाग मानव द्वारा निर्मित प्रदूषण से जूझ रहा है जिसके कारण विभिन पर्यावरणीय समस्याएँ उत्पन हो गयी है। जल, स्थल, वायुमंडल सहित जीवमंडल का सम्पूर्ण पारिस्थितिक तंत्र प्रदूषण के कारण संकट में है। मानवीय प्रदूषण के कारण उत्पन संकट को दूर करने के लिए सरकार द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के माध्यम से देश के नागरिको को जागरूक किया जाता है। आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको बताने वाले है की राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस क्या है ? (National Pollution Control Day), प्रदूषण दिवस 2 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है ? इसका उद्देश्य एवं महत्व क्या है ? साथ ही इस आर्टिकल के माध्यम से आपको प्रदूषण नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन कार्यक्रमों की भी जानकारी प्रदान की जाएगी।
वर्तमान समय में मानवीय कारकों के कारण पर्यावरण में प्रदूषण में निरंतर वृद्धि हो रही है जो की वास्तव में सम्पूर्ण मानव जाति के लिए खतरे की घंटी है। पारिस्थितिक तंत्र के सभी भागों में मानव निर्मित प्रदूषण अपनी पैठ बना चुका है जिसके कारण पारिस्थितिक तंत्र के सभी जीव-जंतुओं एवं वनस्पतियों का अस्तित्व खतरे में पड़ चुका है। प्रदूषण वह स्थित होती है जब किसी भी पारिस्थितिक तंत्र (जल, स्थल, वायु) में विभिन अवयवों की मात्रा निर्धारित संतुलित सीमा से अधिक हो जाती है जिसके कारण संपूर्ण तंत्र का संतुलन बिगड़ जाता है एवं पारिस्थितिक तंत्र का अस्तित्व संकट में आ जाता है। प्रदूषण के कारण पारिस्थितिक तंत्र के विभिन अवयवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं पूरे तंत्र में असंतुलन की स्थित पैदा हो जाती है। प्रदूषण के कारकों के आधार पर इसे विभिन प्रकार से विभाजित किया गया है जिन्हे मुख्यत निम्न प्रकार से बाँटा गया है :- जल-प्रदूषण, वायु-प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्रदूषण के प्रमुख कारक है। मानव निर्मित औद्योगिक गतिविधियों, रसायनों के प्रयोग, खनिज तेल का उपयोग एवं प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुन दोहन के कारण प्रदूषण पैदा होता है।
राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस
राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गँवा दी थी। उन मृतकों को सम्मान देने और याद करने के लिये भारत में हर वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी वर्ष 1984 में 2 और 3 दिसंबर की रात में शहर में स्थित यूनियन कार्बाइड के रासायनिक संयंत्र से जहरीला रसायन जिसे मिथाइल आइसोसाइनेट (एमआईसी) के रूप में जाना जाता है के साथ-साथ अन्य रसायनों के रिसाव के कारण हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, 500,000 से अधिक लोगों की (जो 2259 के आसपास तुरंत मर गये) एमआईसी की जहरीली गैस के रिसाव के कारण मृत्यु हो गयी। बाद में, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये घोषित किया गया कि गैस त्रासदी से संबंधित लगभग 3,787 लोगों की मृत्यु हुई थी। अगले 72 घंटों में लगभग 8,000-10,000 के आसपास लोगों की मौत हुई, वहीं बाद में गैस त्रासदी से संबंधित बीमारियों के कारण लगभग 25000 लोगों की मौत हो गयी। ये पूरे विश्व में इतिहास की सबसे बड़ी औद्योगिक प्रदूषण आपदा के रुप में जाना गया जिसके लिये भविष्य में इस प्रकार की आपदा से दूर रहने के लिए गंभीर निवारक उपायों की आवश्यकता है।
प्रदूषण नियंत्रण दिवस क्यों मनाया जाता है ? इतिहास
प्रदूषण नियंत्रण दिवस का आयोजन नागरिको को पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जागरूक करने एवं इसके प्रबंधन, नियंत्रण एवं समुचित निस्तारण के लिए प्रभावी उपाय करने के सम्बन्ध में जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है। प्रदूषण नियंत्रण दिवस के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जानकारी प्रदान करने के अतिरिक्त इसके पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव, मानवीय एवं औद्योगिक लापरवाही से उत्पन प्रदूषण को नियंत्रित करने एवं सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में बनाये गए विभिन नियमों एवं कानूनों के बारे में नागरिको को जानकारी प्रदान की जाती है। भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस को मनाने की शुरुआत दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी में शुमार भोपाल गैस त्रासदी के बाद हुयी थी। 2 दिसंबर 1984 की रात को मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में यूनियन कार्बाईड इंडिया लिमिटेड नामक कंपनी की कीटनाशक फैक्ट्री से औद्योगिक दुर्घटना के कारण जानलेवा जहरीली गैस मिथाईल आइसोसाइनेट (MIC) का रिसाव हुआ था। इस घटना के कारण भोपाल में हजारों लोग मारे गए थे। भोपाल गैस त्रासदी में जान गवाँने वाले मृतकों की स्मृति में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है।
राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस थीम 2023
राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2022 की थीम पर आगे बढ़ते हुए, इसे व्यापक रूप से गो ग्रीन और ब्रीथ प्योर एयर माना जाता था। हालाँकि, यह याद रखना आवश्यक है कि इस विशिष्ट विषय की आधिकारिक तौर पर उच्च अधिकारियों द्वारा घोषणा नहीं की गई थी। इसके बावजूद, यह उस दिन के महत्व और उद्देश्य से पूरी तरह मेल खाता है। इसके अलावा इस साल की थीम की भी अभी घोषणा नहीं की गई है।
राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, उद्देश्य
राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य नागरिको को पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जागरूक करना है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के माध्यम से सरकार एवं विभिन गैर-सरकारी संस्थानों के द्वारा विभिन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिसके माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण का कारकों, इसके नियंत्रण एवं निस्तारण में लोगों की सहभागिता के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्ययोजना को लागू किया जाता है। साथ ही जन-सहभागिता के अतिरिक्त राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के अवसर पर विभिन नियमों एवं कानूनो के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाता है। पर्यावरण प्रदूषण हेतु प्रभावी उपायों के बारे में भी इस दिवस के अवसर पर विभिन प्रकार की जानकारी साझा की जाती है।
प्रदूषण का मानवीय जीवन पर प्रभाव
प्रदूषण का पारिस्थितिक तंत्र सहित मानवीय जीवन पर घातक प्रभाव होता है। प्रदूषण के कारण पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन उत्पन हो जाता है जिसके कारण विभिन जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। प्रदूषण का पारिस्थितिक तंत्र सहित मानव जीवन पर घातक प्रभाव पड़ता है। इसके कारण विभिन जीवों के खाद्यान एवं आवास पर संकट उत्पन होता है। साथ ही विभिन वैज्ञानिक अनुसंधानो में भी यह बात साबित हो चुकी है है की प्रदूषण ना सिर्फ हृदय, श्वसन एवं तंत्रिका तंत्र सम्बंधित बीमारियों के लिए जिम्मेदार है अपितु यह कैंसर जैसे बीमारियों का भी प्रमुख कारक है। प्रदूषण के कारण लोगो की उम्र में 10 वर्ष तक की कमी सम्बंधित शोध भी प्रकाशित हो चुके है।
प्रदूषण रोकने में हमारी भूमिका
प्रदूषण रोकने में सरकार द्वारा विभिन प्रकार के कार्यक्रमों का सञ्चालन किया जा रहा है। सरकार द्वारा प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए 22 सितम्बर 1974 को सांविधिक संगठन के रूप में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया है। वर्ष 1986 में सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित करके प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्ययोजना लागू की गयी। सक्रिय नागरिको के रूप में देश के निवासियों की जिम्मेदारी है की प्रदूषण रोकथाम के लिए बनाये गए विभिन नियम एवं कानूनों का पालन करके प्रदूषण रोकथाम में सक्रिय भूमिका अदा करें एवं प्रदूषण नियंत्रण में अपना योगदान दे। साथ ही प्रतिदिन के जीवन में विभिन कार्यों के माध्यम से भी हम प्रदूषण
आइए वायु प्रदूषण को कम करने के 10 सर्वोत्तम तरीके।
1. सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना : सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कम वायु प्रदूषण में योगदान देने का एक निश्चित तरीका है क्योंकि यह कम गैस और ऊर्जा प्रदान करता है, यहां तक कि कारपूल भी इसमें योगदान करते हैं। ईंधन और गैस के कम उत्सर्जन के अलावा, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने से पैसे बचाने में भी मदद मिल सकती है। सड़कों पर कम वाहन कम उत्सर्जन में योगदान देंगे। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने में मदद मिलेगी
2. उपयोग में न होने पर लाइट बंद कर दें : रोशनी जो ऊर्जा लेती है वह भी वायु प्रदूषण में योगदान करती है, इस प्रकार बिजली की कम खपत से ऊर्जा की बचत की जा सकती है। पर्यावरण की मदद के लिए ऊर्जा की बचत करने वाली फ्लोरोसेंट रोशनी का उपयोग करें।
3. रीसायकल और पुन: उपयोग करें : रीसायकल और पुन: उपयोग की अवधारणा न केवल संसाधनों का संरक्षण करती है और उनका न्यायिक रूप से उपयोग करती है बल्कि वायु प्रदूषण के लिए भी सहायक है क्योंकि यह प्रदूषण उत्सर्जन को कम करने में मदद करती है। पुनर्चक्रित उत्पाद अन्य उत्पादों को बनाने में कम शक्ति भी लगाते हैं।
4. प्लास्टिक की थैलियों को ना : प्लास्टिक उत्पादों का उपयोग पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है क्योंकि तेल से बनी उनकी सामग्री के कारण उन्हें अपघटित होने में बहुत लंबा समय लगता है। इसके बजाय पेपर बैग का उपयोग एक बेहतर विकल्प है क्योंकि वे आसानी से विघटित हो जाते हैं और पुन: प्रयोज्य होते हैं।
5. जंगल की आग और धूम्रपान में कमी : शुष्क मौसम में कचरे का संग्रह और उसमें आग लगना या सूखे पत्तों में आग लगना वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारक है, इसके अलावा धूम्रपान भी वायु प्रदूषण का कारण बनता है और स्पष्ट रूप से किसी के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाने के साथ-साथ वायु की गुणवत्ता को खराब करता है।
6. एयर कंडीशनर की जगह पंखे का प्रयोग करें : एसी के उपयोग में बहुत अधिक ऊर्जा लगती है और बहुत अधिक गर्मी निकलती है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। पंखे की तुलना में एसी को काम करने में बहुत शक्ति और ऊर्जा लगती है।
7. चिमनियों के लिए फिल्टर का प्रयोग करें : घरों और कारखानों में चिमनियों से निकलने वाली गैस वायु प्रदूषण के लिए बेहद खतरनाक होती है और वायु की गुणवत्ता को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाती है। यदि खपत को कम नहीं किया जा सकता है तो फिल्टर का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए, इससे हानिकारक गैसों के हवा में अवशोषित होने के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी।
8. पटाखों के प्रयोग से बचें : दुख की बात है कि त्योहारों और शादियों के दौरान पटाखों का उपयोग वायु प्रदूषण के सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है, जिससे स्मॉग की एक परत बन जाती है जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। इसलिए पटाखे नहीं चलाने की प्रथा को लागू किया जाना चाहिए।
9. केमिकल वाले उत्पादों के इस्तेमाल से बचें : उत्पाद जो अपने उपयोग में रसायनों का उपयोग करते हैं या तेज गंध करते हैं, जैसे पेंट या इत्र का कम या घर के बाहर उपयोग किया जाना चाहिए। कम रासायनिक सामग्री और जैविक गुणों वाले उत्पादों का उपयोग करने का विकल्प भी हो सकता है।
10. वनीकरण लागू करें : अंतिम लेकिन कम नहीं, जितना संभव हो उतने पेड़ लगाएं और उगाएं। पेड़ लगाने के अभ्यास से पर्यावरण को बहुत लाभ मिलता है और ऑक्सीजन छोड़ने में मदद मिलती है।
भारत में प्रदूषण नियंत्रण पर कानून।
भारतीय सरकार ने पूरे भारत में प्रदूषण के नियंत्रण और रोकथाम के लिये विभिन्न संजीदा नियम और कानून बनाये हैं, जिनमें से कुछ निम्न है:
* 1974 का जल (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम,
* 1977 का जल उपकर (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम,
* 1981 का वायु (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम,
* 1986 का पर्यावरण (संरक्षण) नियम,
* 1986 का पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,
* 1989 का खतरनाक रासायनिक निर्माण, भंडारण और आयात का नियम
* 1989 का खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम,
* 1989 का खतरनाक माइक्रो जीव अनुवांशिक इंजीनियर जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, भंडारण, आयात, निर्यात और भंडारण का नियम,
* 1996 का रासायनिक दुर्घटनाओं (इमरजेंसी, योजना, तैयारी और प्रतिक्रिया) नियम,
* 1998 का जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और संचालन) नियम,
* 1999 का पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक निर्माण और उपयोग नियम
* 2000 का ओजोन क्षयकारी पदार्थ (विनियमन) नियम
* 2000 का ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) का नियम
* 2000 का नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और संचालन) नियम
* 2001 का बैटरियों (मैनेजमेंट और संचालन) नियम।
* 2006 का महाराष्ट्र जैव कचरा (नियंत्रण) अध्यादेश।
* 2006 का पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना नियम।
राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भूमिका।
सभी अच्छे और खराब कार्यों के नियमों और कानूनों की राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (NPCB) या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जाँच की जाती है जो भारत में प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकारी निकाय है। ये हमेशा जाँच करता है कि सभी उद्योगों द्वारा पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों का सही तरीके से उपयोग किया जा रहा है या नहीं। महाराष्ट्र में अपना स्वंय का नियंत्रण बोर्ड है जिसे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) कहा जाता है, ये प्रदूषण नियंत्रण की तत्काल आवश्यकता के रुप में है, क्योंकि ये उन बड़े राज्यों में से एक है जहाँ औद्योगीकरण की दर बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वायु, भूमि या वन विभिन्न प्रकार के प्रदूषण द्वारा तेजी से प्रभावित हो रहे हैं जिन्हें सही तरीके से नियमों और विनियमों को लागू करके तुरंत सुरक्षित करना बहुत जरुरी है।
प्रदूषण आज न केवल भारत, बल्कि पूरी दनिया के लिए नासूर बनता जा रहा है, जिसकी वजह से बढ़ती बीमारियों के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ कई गुना बढ़ता जा रहा है। हवा में मौजूद प्रदूषण के कण न केवल दिल, दिमाग और फेफड़ों पर गंभीर असर डालते हैं बल्कि कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों का भी कारण बन रहे हैं। विशेषज्ञों का मत है कि प्रदूषण से उम्र पर पड़ने वाला प्रभाव धूम्रपान और टीबी जैसी बीमारियों से भी ज्यादा है और अगर प्रदूषण को लेकर WHO के मानकों का सख्ती से पालन किया जाए तो लोगों की उम्र में कई साल की बढ़ोतरी हो सकती है। प्रदूषण किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसी समस्या है, जिससे स्वयं को बचाने के लिए निजी स्तर पर कुछ विशेष नहीं कर सकते, बल्कि यह सामूहिक प्रयास है।