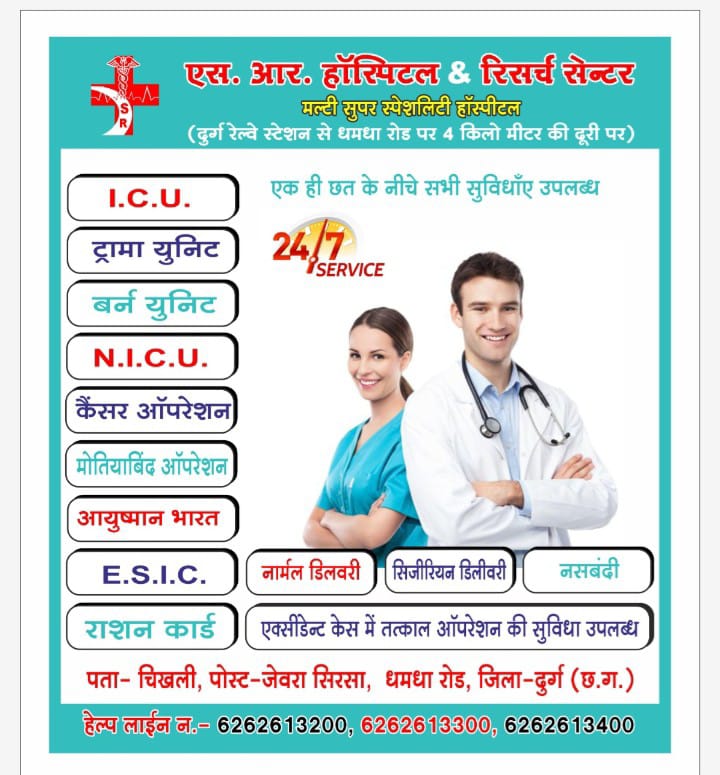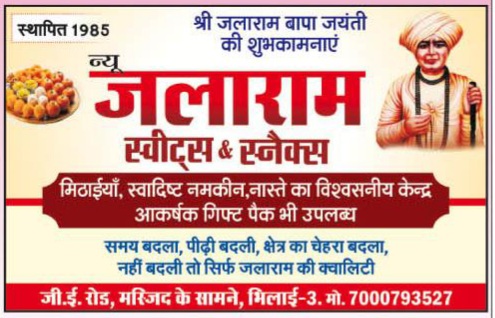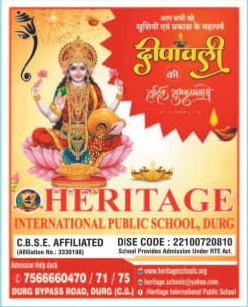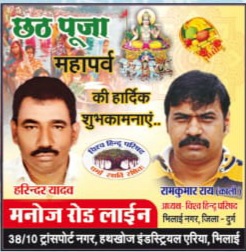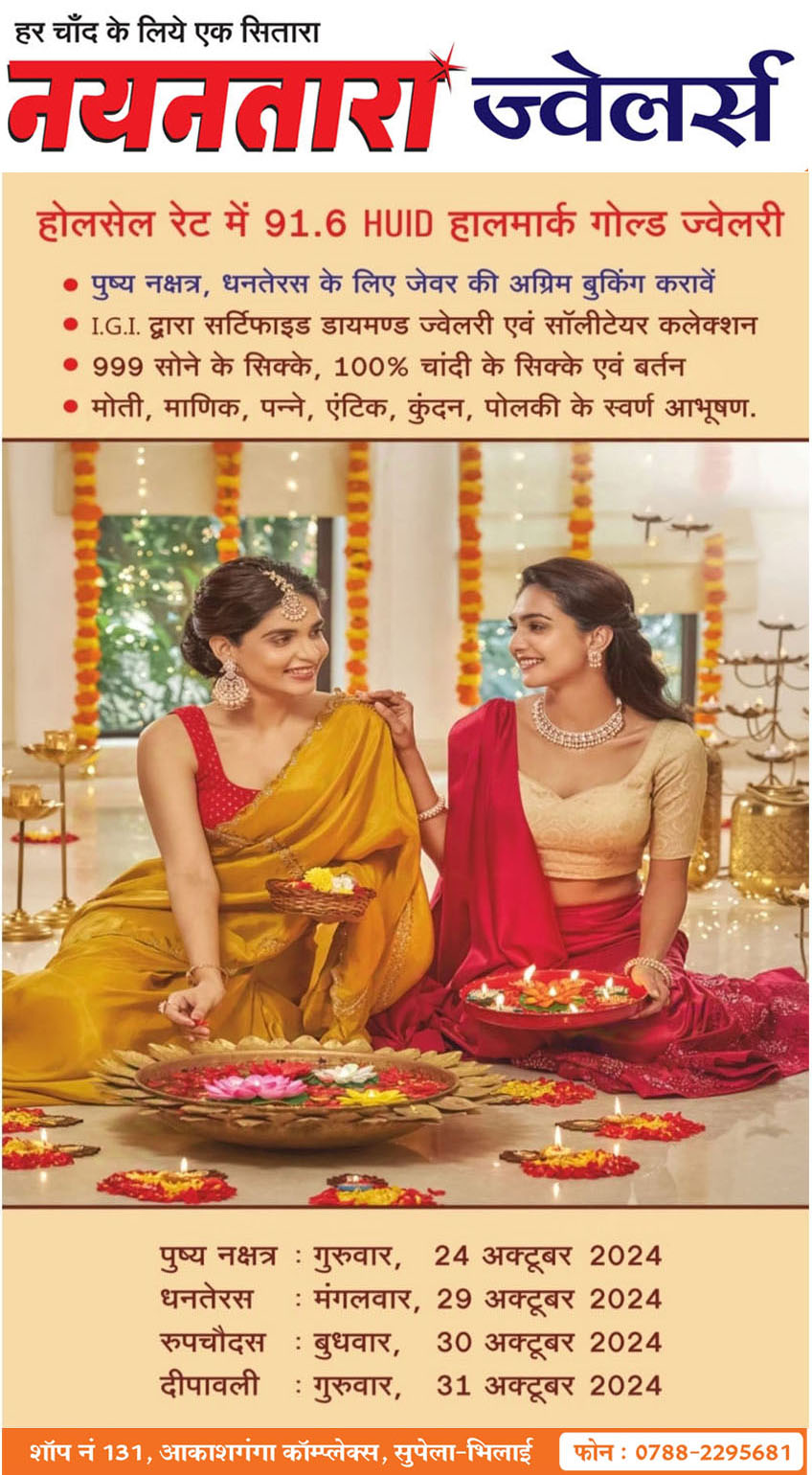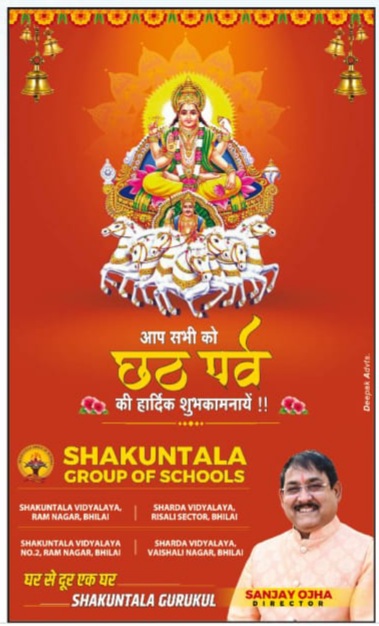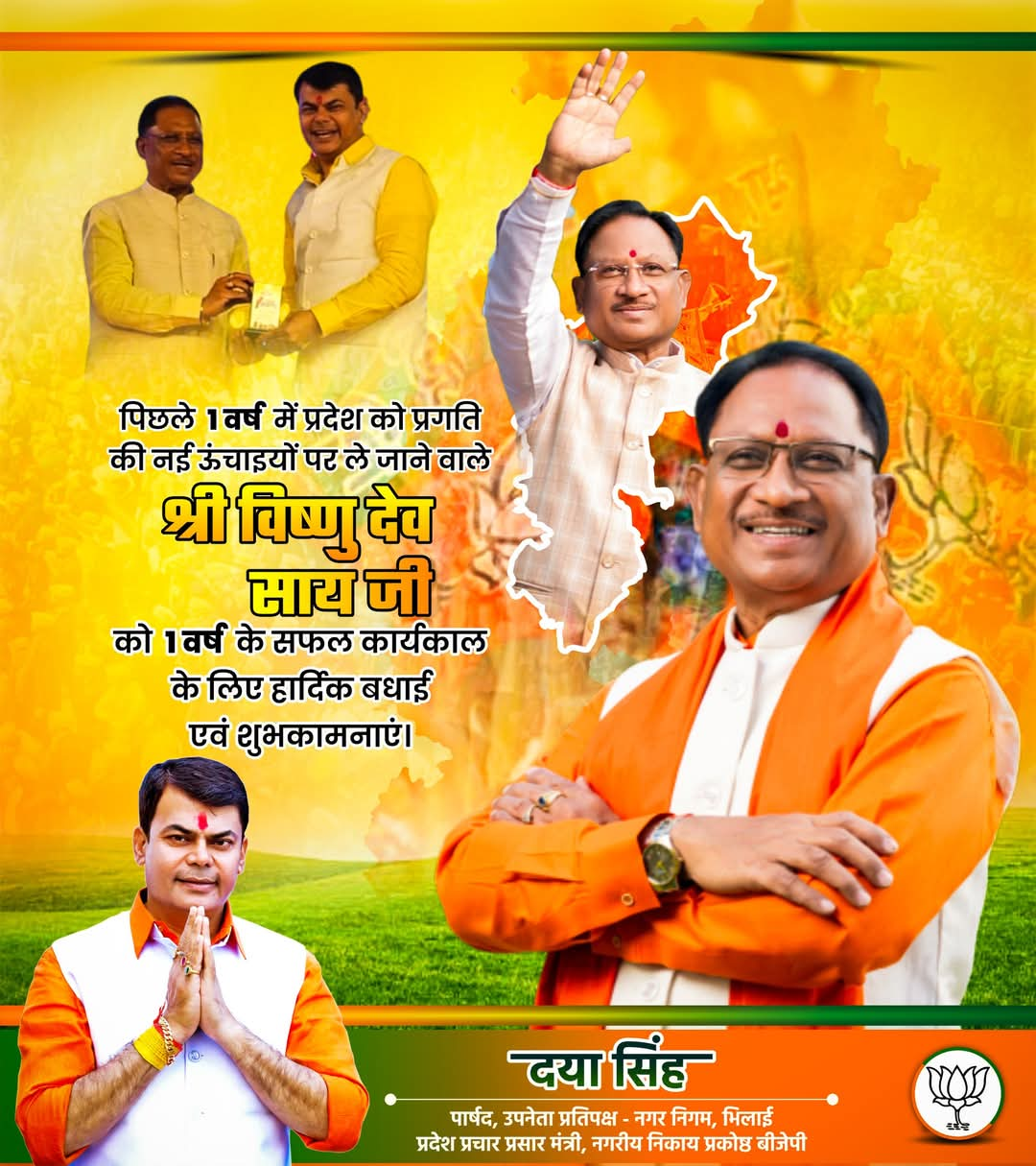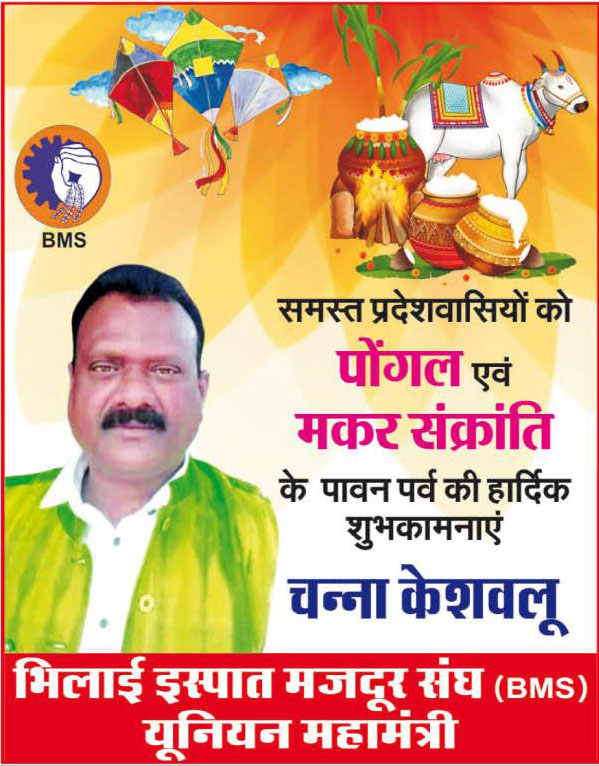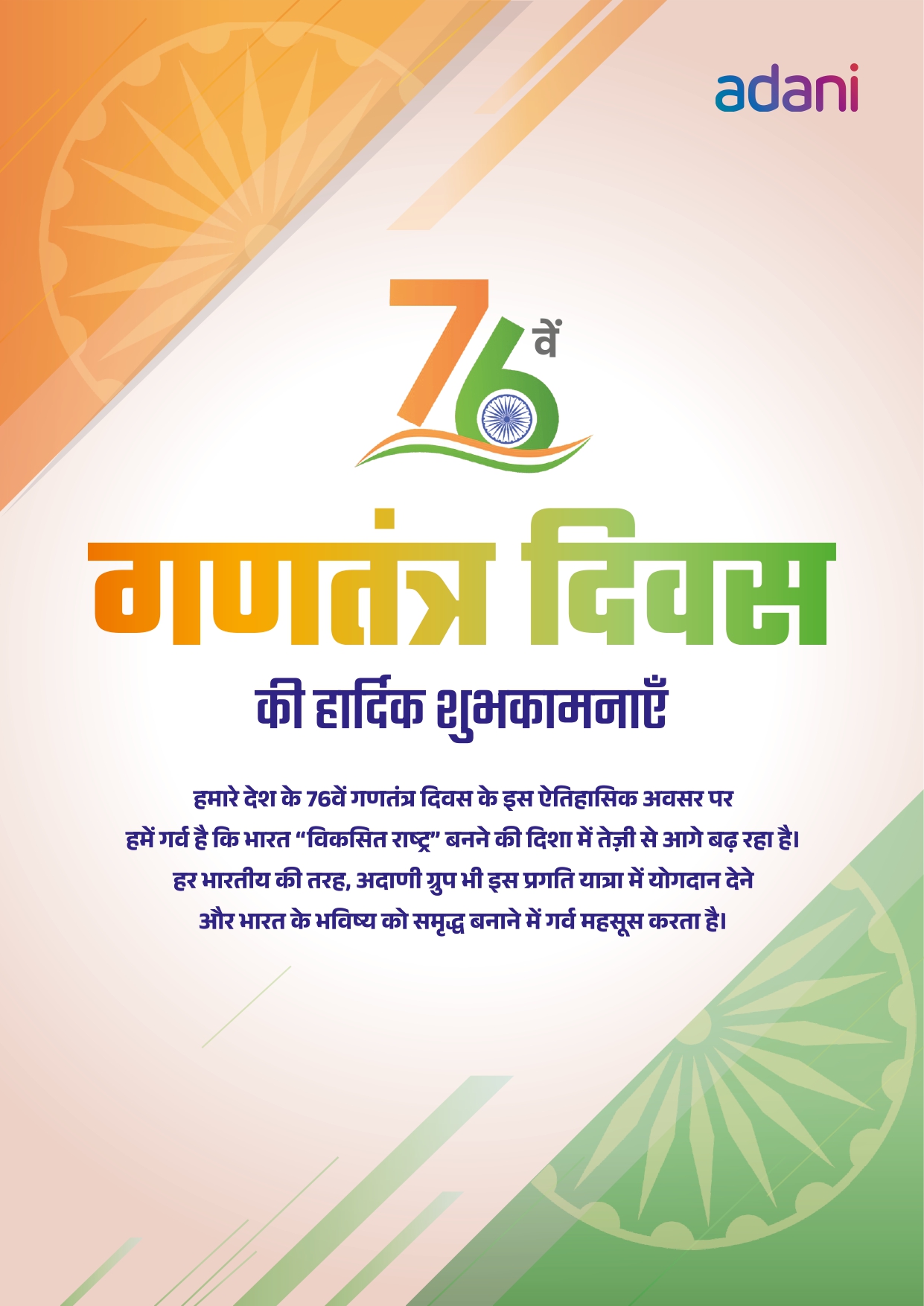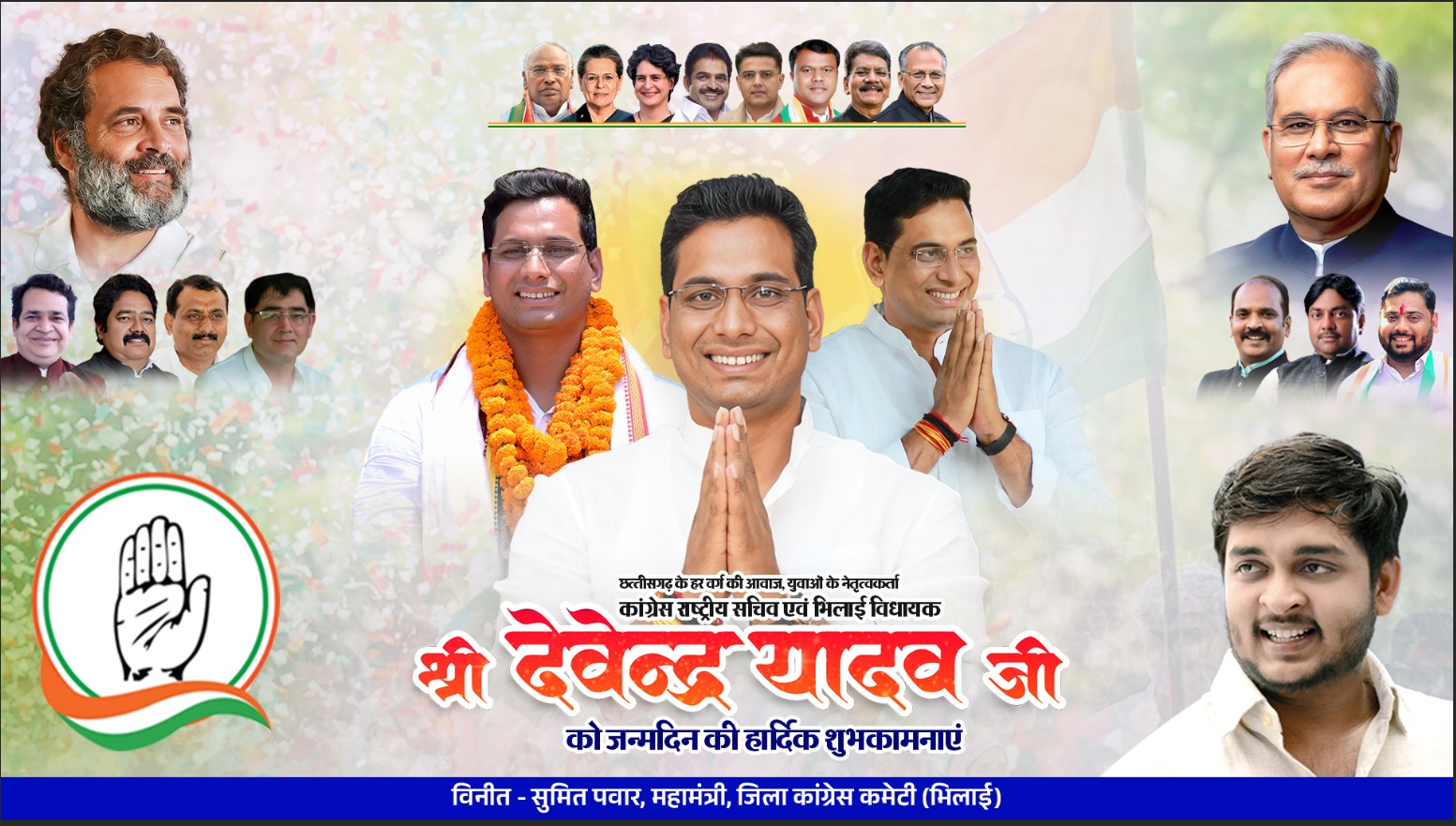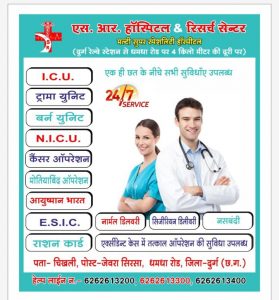प्रतिवर्ष 17 अक्टूबर को पूरे विश्व में गरीबी उन्मूलन के लिए ‘अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस’ मनाया जाता है। यह दिवस गरीबी में रह रहे लोगों के संघर्ष को जानने-समझने और उनकी कठिनाइयों को दूर करने के प्रयासों का मौका देता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत सर्वप्रथम 17 अक्टूबर 1987 को पेरिस के ट्रोकेड्रो में हुई जहां पर 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। यहां पर हजारों लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने गरीबों को मानवाधिकारों का उल्लंघन मानते हुए इसके उन्मूलन हेतु अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। इसके बाद प्रतिवर्ष 17 अक्टूबर को यहां पर विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग गरीबी उन्मूलन की दिशा में एकत्रित होने लगे। वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसे एक अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित किया गया।
गरीबी क्या है?
गरीबी से तात्पर्य ऐसी स्थिति से होता है जब मनुष्य आयऔर अन्य उत्पादक संसाधनों के अभाव में अपनी आजीविका सुनिश्चित नहीं कर पाता। दूसरे शब्दों में गरीबी को एक ऐसे हालात के रूप में देखा जाता है जिसमें व्यक्ति के पास जीवन निर्वाह के लिये बुनियादी ज़रूरतें मसलन रोटी, कपड़ा और मकान भी नहीं होते हैं। इस हालत को चरम गरीबी भी कहा जाता है। गरीबी के अन्य स्वरूपों में भूख और कुपोषण, शिक्षा और अन्य बुनियादी सेवाओं तक सीमित पहुंच, सामाजिक भेदभाव और बहिष्करण, साथ ही निर्णय लेने में भागीदारी का अभाव इत्यादि शामिल है।
गरीब कौन है?
गरीबी को एक ऐसी परिस्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें कोई व्यक्ति अथवा परिवार वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण अपने जीवन निर्वाह के लिये बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है।
अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की 2022 में थीम क्या है?
2022-2023 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम है ‘व्यवहार में सभी के लिए गरिमा’ है। ( ‘Dignity for all in practice’ is the umbrella theme of the International Day for the Eradication of Poverty for 2022-2023)। मानव की “गरिमा” अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। यह अन्य सभी मौलिक अधिकारों का आधार भी बनता है। इसलिए, प्रत्येक की “गरिमा” होनी चाहिए। गरीब लोग अपनी “गरिमा” से वंचित रहते हैं और अपने आदर के साथ समझौता करते हैं। आगे बढ़ने का अर्थ है प्रकृति के साथ अपने संबंधों को बदलना, भेदभाव की संरचनाओं को नष्ट करना और मानव अधिकारों के नैतिक और कानूनी ढांचे पर निर्माण करते रहना। आगे बढ़ने का मतलब है कि गरीबी में रहने वाले लोगों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाता है और उन्हें सामने आने के लिए समर्थन दिया जाता है।
हम एक साथ जो प्रतिबद्धताएं करते हैं
व्यवहार में सभी के लिए गरिमा 2022-2023 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का मुख्य विषय है। मनुष्य की गरिमा न केवल अपने आप में एक मौलिक अधिकार है बल्कि अन्य सभी मौलिक अधिकारों का आधार है। इसलिए, “गरिमा” एक अमूर्त अवधारणा नहीं है: यह प्रत्येक से संबंधित है। आज, लगातार गरीबी में रहने वाले बहुत से लोग अनुभव करते हैं कि उनकी गरिमा को नकारा जा रहा है और उनका अनादर किया जा रहा है। गरीबी को समाप्त करने , ग्रह की रक्षा करने और सभी लोगों को हर जगह शांति और समृद्धि का आनंद लेने की प्रतिबद्धता के साथ , 2030 एजेंडा ने फिर से मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के तहत स्थापित उसी वादे की ओर इशारा किया । फिर भी, वर्तमान वास्तविकता से पता चलता है कि 1.3 बिलियन लोग अभी भी बहुआयामी गरीबी में रहते हैं जिनमें से लगभग आधे बच्चे और युवा हैं।अवसरों और आय की असमानता तेजी से बढ़ रही है और हर साल अमीर और गरीब के बीच की खाई और भी चौड़ी होती जा रही है। पिछले एक साल में, जब लाखों लोग श्रमिकों के अधिकारों और नौकरी की गुणवत्ता के क्षरण के माध्यम से इसे एक और दिन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कॉर्पोरेट शक्ति और अरबपति वर्ग की संपत्ति में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है।गरीबी और असमानता अपरिहार्य नहीं है। वे जानबूझकर किए गए फैसलों या निष्क्रियता का परिणाम हैं जो हमारे समाज में सबसे गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोगों को कमजोर करते हैं और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। गरीबी की मूक और निरंतर हिंसा – सामाजिक बहिष्कार, संरचनात्मक भेदभाव और अशक्तता – अत्यधिक गरीबी में फंसे लोगों के लिए बचने के लिए और उनकी मानवता को नकारने के लिए कठिन बना देती है।COVID -19 महामारी ने इस गतिशील, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के अंतराल और विफलताओं के साथ-साथ संरचनात्मक असमानताओं और भेदभाव के विविध रूपों को उजागर किया जो गरीबी को गहरा और बनाए रखते हैं। इसके।अलावा, जलवायु आपातकाल गरीबी में रहने वाले लोगों के खिलाफ नई हिंसा का गठन करता है, क्योंकि ये समुदाय प्राकृतिक आपदाओं और पर्यावरणीय गिरावट की अधिक लगातार घटनाओं से अनावश्यक रूप से बोझिल होते हैं, जिससे उनके घरों, फसलों और आजीविका का विनाश होता है। इस वर्ष अत्यधिक गरीबी पर काबू पाने के लिए विश्व दिवस की 35वीं वर्षगांठ और गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की 30वीं वर्षगांठ है। यह दिवस गरीबी से पीड़ित लाखों लोगों और उनके दैनिक साहस का सम्मान करता है और आवश्यक वैश्विक एकजुटता और साझा जिम्मेदारी को पहचानता है जो हम गरीबी को मिटाने और सभी प्रकार के भेदभाव का मुकाबला करने के लिए रखते हैं।
पार्श्वभूमि
एक अभूतपूर्व स्तर के आर्थिक विकास, तकनीकी साधनों और वित्तीय संसाधनों की विशेषता वाली दुनिया में, लाखों लोग अत्यधिक गरीबी में जी रहे हैं, यह एक नैतिक आक्रोश है। गरीबी केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि एक बहुआयामी घटना है जिसमें आय की कमी और सम्मान से जीने की बुनियादी क्षमता दोनों शामिल हैं।गरीबी में रहने वाले व्यक्ति कई परस्पर संबंधित और पारस्परिक रूप से मजबूत अभावों का अनुभव करते हैं जो उन्हें अपने अधिकारों का एहसास करने से रोकते हैं और उनकी गरीबी को बनाए रखते हैं, जिनमें शामिल हैं:
* खतरनाक काम की स्थिति
* असुरक्षित आवास
* पौष्टिक भोजन की कमी
* न्याय तक असमान पहुंच
* राजनीतिक शक्ति की कमी
* स्वास्थ्य देखभाल तक सीमित पहुंच
* दिन के लिए पृष्ठभूमि पर और पढ़ें
संबंधित संगठन और जानकारी
* इंटरनेशनल मूवमेंट एटीडी फोर्थ वर्ल्ड।
* अत्यधिक गरीबी पर काबू पाना।
* 17 अक्टूबर के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति।
* गरीबी उन्मूलन के लिए संयुक्त राष्ट्र का तीसरा दशक।
गरीबी उन्मूलन के लिए तीसरे दशक को लागू करना
जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गरीबी उन्मूलन के लिए तीसरे दशक की शुरुआत कर रहा है, 2013 में अनुमानित 783 मिलियन लोग प्रति दिन $ 1.90 से कम पर रहते थे, जबकि 1990 में 1.867 बिलियन लोग थे। विकासशील देशों में आर्थिक विकास 2000 के बाद से उल्लेखनीय रहा है। उन्नत देशों की तुलना में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में तेज वृद्धि। इस आर्थिक विकास ने गरीबी में कमी और जीवन स्तर में सुधार को बढ़ावा दिया है। रोजगार सृजन, लैंगिक समानता, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सुरक्षा उपाय, कृषि और ग्रामीण विकास, और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन जैसे क्षेत्रों में भी उपलब्धियां दर्ज की गई हैं।
गरीबी से संबंधित कुछ प्रमुख वैश्विक आंकड़े
‘सतत् विकास लक्ष्य’- 1 में गरीबी की समाप्ति में (NO POVERTY) को रखा गया है, जिसका लक्ष्य गरीबी को इसके सभी रूपों में हर जगह से समाप्त करना है। वैश्विक और राष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद गरीबी उन्मूलन एक प्रमुख चुनौती बना हुआ है जिसके कुछ आकड़ें निम्न है-
* 2021 में COVID-19 महामारी ने 143 से 163 मिलियन लोगों को गरीबी में धकेलने की संभावना है।
* COVID-19 महामारी से 2019 की तुलना में 2020 में 8.1% (8.4% से 9.1% तक) गरीबी बढ़ने की उम्मीद है।
* निम्न और उच्च मध्यम आय वाले देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में 2.3 प्रतिशत अंक की गरीबी दर में वृद्धि होने का अनुमान है।
* अनुमानित नए गरीबों में से लगभग आधे दक्षिण एशिया में होंगे, और एक तिहाई से अधिक उप-सहारा अफ्रीका में होंगे।
* मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में, 2015 और 2018 के बीच अत्यधिक गरीबी दर लगभग दोगुनी होकर 3.8 प्रतिशत से 7.2 प्रतिशत हो गई, जो सीरियाई अरब गणराज्य और यमन गणराज्य में संघर्षों से प्रेरित है।
* वर्तमान अनुमानों से संकेत मिलता है कि 2020-21 में लगभग सभी अर्थव्यवस्थाओं में साझा समृद्धि में तेजी से गिरावट आई है, क्योंकि पूरे आय वितरण में महामारी का आर्थिक बोझ महसूस किया जाता है।
* पिछले तीन दशकों में वैश्विक गरीबी में कमी के लक्ष्य की दिशा में COVID-19 पहले से ही सबसे खराब उलटफेर रहा है।
* 2015 में दुनिया में 736 मिलियन अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा 1.90डॉलर/ प्रतिदिन से नीचे जीवन गुजर बसर कर रहे थे।
* 2018 में, दुनिया के लगभग 8 प्रतिशत श्रमिक और उनके परिवार अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा (1.90डॉलर/ प्रतिदिन) से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे थे।
* गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले अधिकांश लोग दो क्षेत्रों से संबंधित हैं: दक्षिणी एशिया और उप-सहारा अफ्रीका;
* अक्सर छोटे, संवेदनशील और संघर्ष से प्रभावित देशों में उच्च गरीबी दर पाई जाती हैं;
* 2018 तक, दुनिया की 55 प्रतिशत आबादी के पास सामाजिक सुरक्षा के लिए नकद सहायता तक पहुंच नहीं थी;
* विकासशील देशों में अनुमानित 1.2 बिलियन लोग अभी भी अत्यधिक गरीबी में रहते हैं;
* मध्यम गरीबी (प्रति दिन $ 2 पीपीपी से कम पर रहने वाले) में बहुत धीमी गति से गिरावट आई है; जबकि कई अत्यधिक गरीबी से बाहर हुए हैं लेकिन पुनः उनके अत्यधिक गरीबी वाली श्रेणी में शामिल होने की आशंका बनी हुई है;
* चरम और मध्यम गरीबी दोनों ही मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हैं और दुनिया के 78 प्रतिशत गरीब ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं जोकि अधिकांश कृषि पर निर्भर हैं;
* गरीबों के पास अच्छे काम के अवसर कम है क्योंकि अधिकांश ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां उत्पादकता कम है, स्थानीय आर्थिक गतिविधि अपर्याप्त है, बेरोजगारी दर उच्च है एवं नौकरियों की प्रकृति असुरक्षित हैं;
* गरीबी ने कई बच्चों को श्रम बाजार में धकेल दिया। दुनिया भर में लगभग 60 प्रतिशत बाल श्रम कृषि क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहां बच्चे अक्सर खतरनाक परिस्थितियों में काम करते हैं, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन की संभावना खतरे में पड़ जाती है;
* गरीबी लैंगिक अंतराल को बढ़ा देती है क्योंकि गरीबों के बीच लैंगिक अंतराल अक्सर ज्यादा होता है। उदाहरण के लिए, ग़रीब महिलाओं और पुरुषों के बीच स्कूली शिक्षा के वर्षों में अंतराल, गैर-ग़रीबों के मुकाबले दोगुने से अधिक है;
स्रोत: विश्व बैंक
क्या है गरीबी के मुख्य कारण?
* तेजी से बढ़ती जनसंख्या का दबाव:
* अशिक्षा एवं निम्न मानव विकास:
* लगातार बढ़ती बेरोजगारी:
* देशों में पूंजी की कमी:
* अल्प विकास/ अल्पविकसित अर्थव्यवस्था:
* मूल्य में वृद्धि:
* अर्थव्यवस्था का पारंपरिक स्वरूप
* पर्याप्त कौशल विकास का ना होना:
* उद्यमिता का विकास न होना:
* समुचितऔद्योगीकरण का अभाव:
* पिछड़ी सामाजिकसंस्थाएं:
* भ्रष्टाचार:
* आधारभूत संरचना की कमी:
* भूमि और दूसरी संपत्तियों का असमान वितरण
* गरीबी का दुष्चक्र
भारत में गरीबी से संबंधित आंकड़े
विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक़ भारत में 2030 तक ग़रीबी कम होने के आसार नज़र आ रहे हैं। भारत 2030 तक लगभग 25 मिलियन परिवारों को ग़रीबी रेखा से ऊपर लाने में सफल होगा। और इस तरह गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों की हिस्सेदारी 15 फीसदी से घटकर महज़ 5 फीसदी रह जाएगी।साल 2011 की जनगणना के आधार पर देश की क़रीब 22 फीसदी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जी रही है। ये भारत सरकार का आधिकारिक आंकड़ा है। वर्ल्ड इनइक्वैलिटी लैब के मुताबिक़ भारत में महज़ 1 फीसदी लोगों की आय साल 1980 से 2019 के बीच छह फीसदी से बढ़कर 21 फीसदी हुई है। इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि ग़रीबी कम होने के साथ-साथ आर्थिक असमानता में बढ़ोत्तरी हुई है। आपको बता दें कि वर्ल्ड इनइक्वैलिटी लैब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आर्थिक असमानता पर शोध करने वाली एक संस्था है।वक़्त के साथ गरीबी में कमी तो आयी है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में कमी की दर अभी भी धीमा ही है। शहरी क्षेत्रों की 13.7% के मुक़ाबले ग्रामीण भारत की लगभग 26% आबादी गरीब है।
ग़रीबी रेखा निर्धारण से जुड़ी समितियां
भारत में गरीबी रेखा को परिभाषित करना हमेशा से ही एक विवादित मुद्दा रहा है। साल 1970 के मध्य में पहली बार इस तरह की गरीबी रेखा का निर्धारण योजना आयोग द्वारा किया गया था। इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमश: एक वयस्क के लिए 2,400 और 2,100 कैलोरी की न्यूनतम दैनिक ज़रुरत को आधार बनाया गया था।
* 2014 तक गरीबी रेखा का निर्धारण ग्रामीण इलाकों में 32 रुपए प्रतिदिन और कस्बों तथा शहरों में 47 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से निर्धारित की गई थी।
* 2017 में नीति आयोग द्वारा गरीबी दूर करने हेतु प्रस्तुत एक विज़न डॉक्यूमेंट में 2032 तक गरीबी दूर करने की योजना तय की गई थी।
* देश में गरीबों की यथार्थ आकलन के लिये नीति आयोग ने अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में एक टास्क फ़ोर्स का गठन किया था।
* वर्तमान में नीति आयोग भारत सरकार की आधिकारिक एजेंसी है, जो राज्यों में और पूरे देश के लिए समग्र रूप से गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का आकलन करने का काम करती है।
* गरीबी रेखा से जुड़ी प्रमुख समितियों का कालक्रम:
# अलघ समिति (1979)
# लकड़ावाला समिति (1993)
# तेंदुलकर समिति (2009)
# रंगराजन समिति (2012)
भारत में गरीबी उन्मूलन एवं जीवन स्तर को उठाने हेतु प्रमुख योजनाएं
साल 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में तेज़ी से सुधार हुआ है। ग़रीबी उन्मूलन के लिए सरकार ने कई योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरुआत की है। इसमें रोज़गार सृजन कार्यक्रम, बीमा कार्यक्रम, आय समर्थन कार्यक्रम, रोज़गार गारंटी और आवास योजना जैसे क़दम शामिल हैं। कुछ योजनाओं पर एक नज़र –
* राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम।
* राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना।
* ग्रामीण श्रम रोज़गार गारंटी। कार्यक्रम।
* राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना।
* शहरी गरीबों के लिये स्वरोज़गार कार्यक्रम।
* प्रधानमंत्री जन धन योजना:
* किसान विकास पत्र योजना:
* दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना।
* महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम:
* प्रधान मंत्री श्रम-योगी मानधन (PMSYM) पेंशन योजना
* अटल पेंशन योजना
* प्रधानमंत्री आवास योजना:
* राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना:
* प्रधानमंत्री मुद्रा योजना:
* आयुष्मान भारत:
* प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि:
भारत में गरीबी उन्मूलन से जुड़ी कुछ प्रमुख चुनौतियां:
अभी भी भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण एक प्रमुख चुनौती है। विभिन्न सारी समितियों ने अपने अलग-अलग आधार और मापदंड दिए हैं लेकिन कुल मिला जुला कर अभी कोई एक ऐसी मान्य परिभाषा नहीं है जिससे गरीबों को परिभाषित कर उन्हें लक्षित किया जा सके।गरीबी उन्मूलन के लिए संसाधनों का पर्याप्त ना होना एक प्रमुख चुनौती है। सरकार के द्वारा गरीबी उन्मूलन की दिशा में अत्यधिक खर्च बढ़ाने एवं उसके उपरांत और राजकोषीय संतुलन को बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। गरीबी उन्मूलन की दिशा में भ्रष्टाचार भी एक प्रमुख समस्या है क्योंकि प्राय: यह देखा गया है की योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थी तक योजनाओं की पहुंच नहीं हो पाती। उचित कार्यान्वयन और सही लक्ष्यीकरण का अभाव। योजनाओं का अतिव्यापीकरण के कारण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाते। लगातार बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में संसाधनों का विकास ना हो पाना।
गरीबी उन्मूलन हेतु सुझाव
* वैज्ञानिक तरीके से एक गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाए जिससे गरीबों की पहचान की जा सके एवं उन्हें सरकारी योजना द्वारा लक्षित किया जा सके।
* ग्रामीण गरीब जनसंख्या में बहुसंख्यक छोटे किसान हैं शामिल है जो अधिकांश वैश्विक खाद्य उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से हमें कृषि उत्पादकता में सुधार, संसाधनों और प्रौद्योगिकियों समेत बाजार तक पहुंच में उनकी मदद करना होगा। एक शोध के अनुसार विकासशील देशों में सामान्य जीडीपी वृद्धि की तुलना में कृषि के विकास से गरीबी उन्मूलन पर 5 गुना अधिक प्रभाव होता है।
* गरीबी को कम करने के लिए पारिस्थितिक और संसाधन की स्थिरता की आवश्यकता है। जब तक उत्पादन के तरीके और खपत के पैटर्न अधिक टिकाऊ नहीं होंगे, तब तक खाद्य उत्पादन में वृद्धि से भूमि क्षरण, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और जैव विविधता की हानि होगी। छोटे किसानों को खाद्य प्रणालियों निरंतर बदलाव के लिए प्रौद्योगिकियों और बुनियादी ढांचे तक सर्वसुलभ पहुंच सुनिश्चित करना होगा
* ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी कम करने के लिए रोजगार का विविधीकरण करने हेतु गैर कृषि गतिविधियों को बढ़ाना होगा। गैर-कृषि गतिविधियों का विकास अक्सर कृषि विकास द्वारा संचालित होती हैं और यह स्थानीय रोजगार सृजन को प्रोत्साहित कर सकती हैं;
* शिक्षा के क्षेत्र में लिंग अंतराल को समाप्त करते हुए महिलाओं को उत्पादक संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने से आय का स्तर बढ़ाया जा सकता है विशेषकर कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में;
* आधारभूत अवसंरचना में सुधार (जैसे सड़क, बिजली और बिजली बाजारों से जुड़ाव)ग्रामीण शहरी संपर्क को मजबूत करते हैं जिससे ना केवल गैर-कृषि में उत्पादकता बढ़ती है बल्कि रोजगार के पर्याप्त अवसर भी सृजित होते हैं
* बेहतर सामाजिक सुरक्षा गरीबों को बेहतर जोखिम प्रबंधन, उनकी आजीविका में सुधार करने और उनके बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ाने में मदद कर सकती है। इस प्रकार यह न केवल गरीबी और भूख के उन्मूलन में तेजी लाने में मदद करेगा, बल्कि जीवन की संभावनाओं में असमानता को भी कम करेगा;
* ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण में शुरुआती निवेश आवश्यक हैं। कई ग्रामीण युवा आर्थिक संभावनाओं की तलाश में पलायन करते हैं। अतः स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को उन्नत और विविधता प्रदान करते हुए युवाओं को कौशल प्रदान किया जाए जिससे इनके आर्थिक संभावनाओं की स्थिति में सुधार हो सके।
* बेहतर शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास और श्रम की उत्पादकता में वृद्धि हेतु आवश्यक है कि स्वस्थ और संतुलित आहार उपलब्ध करवाया जाए।
* सरकारी योजना से भ्रष्टाचार हटाने हेतु नवीनतम तकनीकों का सहारा लिया जाना चाहिए।
वैश्विक गरीबी पर COVID-19 का प्रभाव
प्रति व्यक्ति घरेलू आय या खपत में संकुचन के माध्यम से वैश्विक मौद्रिक गरीबी पर COVID-19 के संभावित अल्पकालिक आर्थिक प्रभाव के अनुमान बताते हैं कि COVID-19 संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य के लिए 2030 तक गरीबी को समाप्त करने के लिए एक वास्तविक चुनौती है क्योंकि वैश्विक गरीबी 1990 के बाद पहली बार वृद्धि हो सकती है और, गरीबी रेखा के आधार पर, इस तरह की वृद्धि गरीबी को कम करने में दुनिया की प्रगति में लगभग एक दशक के उलट का प्रतिनिधित्व कर सकती है। कुछ क्षेत्रों में प्रतिकूल प्रभावों के परिणामस्वरूप गरीबी का स्तर 30 साल पहले दर्ज किए गए स्तर के समान हो सकता है। 20 प्रतिशत आय या उपभोग संकुचन के सबसे चरम परिदृश्य के तहत, गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या 2018 के लिए नवीनतम आधिकारिक रिकॉर्ड किए गए आंकड़ों के सापेक्ष 420-580 मिलियन तक बढ़ सकती है।